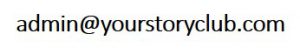कभी – कभी मैं सोचा करती हूँ ,
कि ज़माने पर मैं इतनी मोहताज क्यूँ ?
खुद चलने की मुझमे हिम्मत गर नहीं ,
तो ज़माना मेरे साथ चले , ऐसी ख्वाईश क्यूँ ?
खुद आगे बढ़ने से ही तो मिलती हैं मंजिले ,
खुद आगे चलने से ही तो पूरी होती हैं हसरते ,
फिर क्यूँ ना मैं खुद चलके , खुद को आबाद करूँ ?
फिर क्यूँ ना मैं आगे बढ़ , अपनी मंजिलों को तय करूँ ?
एक दिन तो ऐसा ज़रूर आयेगा ,
जब ये ज़माना मुझ पर तरस खायेगा ,
मैं बढ़ती रहूँगी आगे तब भी बेधड़क ,
क्योंकि मिलेगी मुझे तब नई एक सड़क |
उस सड़क पर चलके मैं इतराऊँगी ,
अपनी कामयाबी के नए गीत गुनगुनाऊँगी ,
तब होगा मेरा इस ज़माने से फिर एक संघर्श ,
जब ज़माने और मुझमे ना होगा कोई स्पर्श |
मैने ज़माने को तब पीछे छोड़ दिया होगा ,
और ज़माने से नाता सब तोड़ दिया होगा ,
वो फिर भी मेरे करीब आयेगा ,
मुझे अपनी मीठी – मीठी बातों में फुसलायेगा |
वो कहेगा मुझे फिर से अपने संग चलने को ,
वो कहेगा मुझे फिर से अपने संग मरने को ,
मैं सोच में फिर से तब पड़ जाऊँगी ,
कभी खुद पे , कभी ज़माने पे तरस खाऊँगी |
ज़माने से आगे बड़ना तब मुझे गंवारा ना होगा ,
मेरी धमनियों में बहते लहू का तब कोई सहारा ना होगा ,
मैं फिर से उस सहारे को पकड़ लाऊँगी ,
और ज़माने के संग चलके मुसकाऊँगी |
अब ज़माने से होगा मेरा दोस्ताना ,
मैं आगे भी बढ़ी गर तो साथ उसने है निभाना ,
इसी साथ को पाने की खातिर मैं अब तक इतना दौडी थी ,
खुद आगे चलने की ख्वाईश में कहीं ज़माने को दोष देती थी |
अब हर दोष को मैने गले लगाया ,
ज़माने के साथ चलने में ही एक संतोष है पाया ,
क्योंकि ना मैं और ना ही ये ज़माना होंगे कभी इधर -उधर ,
फिर क्यूँ बेवजह मैं भी करूँ इस ज़माने की फिकर ||
–END–