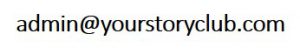Hindi Moral Story – Conscience
Photo credit: earl53 from morguefile.com
कभी – कभी आदमी का आत्मविश्वास इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अहम् की सीमा को छूने लगता है । यह मेरा अहंकार ही था कि मै अपने ब्यवहार को बहुत ही संयत, संतुलित और संशयरहित समझता था । लेकिन उस दिन एक बहुत ही साधारण, अतिसाधारण औरत ने मेरे इसी अहं की परतों को उघेड़कर रख दिया।
मेरा तबादला रूरल पोस्टिंग के तहत उस कस्बेनुमा आदिवासी बहुल इलाके में हो गया था । मैं अपने इस तबादले से बहुत ही खिन्न था । लेकिन बैंक की नौकरी में इसके लिए तो तैयार रहना ही पड़ेगा । यही सोचकर मन मसोसकर रह जाना पड़ा था । पत्नी और बच्ची को शहर में छोड़कर वहाँ जाना एक तरह से उनकी असुरक्षा के बारे में सोचकर खुद ही असुरक्षा के घेरे में घिर जाने जैसा ही था । हालाँकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरी पत्नी हमारे पांच साल के बच्चे सहित शहर में मेरे बिना भी रह सकने में सक्षम थी। लेकिन जब कोई अपनी आँखों से दूर, वह भी पहली बार होता हो तो स्वयं में असुरक्षा का भाव अधिक गहरा हो जाता है । यह शायद अधिक लगाव और अपने चाहने वाले को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करने की इच्छा के कारण भी होता है।
शहर में बैंक कॉलोनी में घर होने के कारण अड़ोस – पड़ोस में भी मेरे पुराने साथी लोग रहते थे । इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। किसी ही आपद्काल में अचानक किसी भी मदद के लिए हर कोई तैयार था। फिर भी मन की मोटी परतों के बीच ममता और वात्सल्य का स्रोत ऐसे समय में ज्यादा प्रवाहमान होने लगता है। पत्नी ने बार – बार आश्वासन दिया था, ‘कोइ चिंता की बात नहीं है, आप आराम से चिंतामुक्त होकर जाइए ।’ मैं भी तो वीक एंड में वहाँ जाने ही वाला था । मुख्य शहर से पांच घंटे की दूरी पर ही तो था वह क़स्बा जहां मेरी पोस्टिंग हुई थी।
वह क़स्बा पहाड़ों से घिरा था .. पहाड़ पेड़ों और झाड़ियों से आच्छादित थे । पहाड़ों से नीचे उतरती झरनों के जल की धवल रेखा ऐसी प्रतीत होती थी, जैसे प्रकृति ने वन देवी के गलें में चांदी का नेकलेस डाल दिया हो । चारो तरफ हरियाली ही हरियाली । प्रकृति ने अपने रंग खोलकर बिखेर दिए थे … दोनों तरफ ऊँचे – ऊँचे पेड़ों के बीच पतली – सी सड़क सरकती चली गई थी । इसी सड़क के दोनों ओर दुकाने थी, सारी चीजों की । किराना सामान से लेकर स्टेशनरी, कास्मेटिक, कपडे, गारमेंट्स और अंडरगार्मेंट्स सभी चीजों की दुकानें उतनी ही जगह में सिमटी हुई थी, सड़क के दोनों ओर..
क़स्बा शांत था, बिलकुल नीरव, लेकिन यह शान्ति मरघट की शान्ति नहीं थी, यह जीवंत शान्ति थी, ऊपर – ऊपर शान्ति, अंदर जीवन साँसें लेता हुआ, हिलोरे लेता हुआ, मल्हार गाता हुआ…
सड़क के किनारे ही स्कूल की नई ईमारत बन रही थी । इसलिए कभी – कभी ट्रकों के घों – घों कर चलने आवाज़ आ जाती थी । इमारत बनाने के लिए शहर से ईंटों की धुलाई हो रही थी । थोड़ी देर घर्र-घर्र की आवाज़ आती, ट्रक से ईंटें उतारी जातीं, फिर ट्रक शहर की ओर वापस चले जाते, फिर सबकुछ वैसे ही शांत, अंदर जीवन जीवंत, मुस्कराता, हँसता, खिलखिलाता…
स्कूल में ड्रेस में जाते हुए बच्चे, उनमें अधिकांश आदिवासी बच्चे बहुत अच्छे लगते, लगता था अब देश में शिक्षा सर्वत्र विस्तार पाएगी और सर्व – सुलभ हो जाएगी।
मैं प्रकृति के निकट सानिध्य की लालसा से सुबह उठकर सड़क के किनारे – किनारे पेड़, जो अपनी गर्दन उठाये आसमान को छूने की जिद में, बढ़कर काफी ऊँचे हो गए थे, उनके बीच छनकर आती सूर्य की किरणों की लुकाछिपी को देखने निकल जाता … मन एक अनुपम, अलौकिक, अह्लाद से भर जाता था । इसी दृश्य को निहारते हुए खो जाने का मन करने लगता था ।
भूल ही जाता कि मेरी पत्नी और बच्चा यहाँ से दूर शहर में हैं और मैं यहां अकेले हूँ । उनसे मोबाइल पर बातें हो जाया करती थीं । मैं सुबह – सुबह चलकर सड़क के उस छोर तक जरूर जाता जहां झरना पहाड़ों के ढलानों से नीचे उतरता था और सड़क पर बनी पुलिया के नीचे से निकल जाता था । छल – छल करती झरनों की मधुर ध्वनि, पेड़ों से छनकर आती सुबह की धूप और चिड़ियों का कलरव एक अद्भुत संगीतमय वातावरण का सृजन करते थे। छायावादी कवि पंत जी की कविता ‘ग्राम युवती’ की ग्राम्या की कल्पना ने ऐसे ही वातावरण में मूर्त रूप धारण किया होगा:
उन्मद यौवन से उभर
घटा – सी नव आषाढ़ की सुन्दर,
अति श्याम चरण,
श्लथ, मंद, चरण,
इठलाती आती ग्राम युवती,
वह गजपति
सर्प डगर पर !
सरकाती – पट,
खिसकाती – लट,_
शर्माती झट
वह नमित दृष्टि से देख उरोजों के युग – घट !
हंसती खलखल,
अबला चंचल
ज्यों फूट पड़ा हो स्रोत सरल,
भर फेनोज्ज्वल दशनों से अधरों के तट !
मेरा शहरी मन तो इस सुदूर क्षेत्र में आकर कविमन में बदलने लगा था । इस बदलाव का भी अजीब आनंद था । इसकी अनुभूति, इस आनंद को अन्दर तक उतारनेवाले को ही हो सकती है, बाकी लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकती ।
मेरे साथ ही बैंक के दो और कर्मचारी रहते थे, उसी बैंक के बगल में जो बैंक ने ही किराए पर लेकर हमलोगों को दे दिया था । वहाँ सबों ने मिलकर एक भोजन बनानेवाला रसोइया रखा हुआ था जो उस डेरे के सारे काम भी करता था और रसोई भी बनाता था । खाने लायक भोजन मिल जाता था, इससे अधिक की इच्छा करना बेकार था ।
किराना सामान तो बगल के स्टोर से ही मोबाइल पर आर्डर कर देने से डेरे पर पहुंचा देते थे । सिर्फ हरी सब्जियों के लिए थोड़ी दूर पर डेली मार्किट तक जाना पड़ता था । डेली मार्किट में रोज ही शाम को ताजा हरी – हरी सब्जियों का बाजार हर दिन लगता था । बाजार शाम होने के ठीक पहले सिमट जाता था क्योंकि बाजार में सब्जियां और अन्य चीजे बेचने वालों को दूर दराज के अपने गांव तक भी तो पहुँचना होता था। सब्जियां रोज या एक दिन बीच करके लाने की जिम्मेवारी मेरी थी। या यों कहिए कि वो जिम्मेवारी मैंने खुद ली थी ताकि मैं अपनी पसंद की सब्जियां ला सकूँ और शाम के पहले भी थोड़ा टहलना हो जाय करे। मैं इस कार्य में योगदान देने में अपनी प्रन्नता महसूस करता था।
उस दिन भी मैं ऑफिस के काम निपटाकर शाम होने के पहले ही सब्जियां लाने निकल गया था। मैं हरी सब्जियां देख रहा था। थोड़ी ताजी सब्जियों को देखने की इच्छा से मैं थोड़ा अंदर तक चला गया। एक जगह एक आदिवासी महिला थोड़ी मैली – कुचैली साड़ी में बिलकुल ताजी सब्जी टोकरी में लिए हुए शांत बैठी थी। उसके बगल में एक पांच साल का बच्चा भी खड़ा था । महिला जो साड़ी लपेटे थी उससे उसकी नंगी बांहे बाहर थी। वह उन्ही हाथों से सब्जी तौल कर ग्राहकों को देती थी। पैसे का हिसाब वह बच्चा भी करता था। उसकी साड़ी के अंदर उसके ब्लाउजरहित और कंचुकीरहित युग कलश अपने उत्तुंग शिखरों सहित बाहर झांकने को उद्धत प्रतीत हो रहे थे। पंत जी की ‘ग्राम युवती” कविता की ग्राम्या जैसे सामने बैठी हो।
परन्तु मेरे आकर्षण का कारण उस ग्राम युवती का उद्दाम यौवन नहीं बल्कि उसकी अन्य टोकरियों की अपेक्षा ताजी सब्जियां थी। इसमें मैं अपना मनोभाव छुपाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उसके सारे बाल काले और घने थे। उसकी केशराशि उसके प्राकृतिक, निष्कलुष और निशंक सौंदर्य को और भी बढ़ा दे रहे थे। इस इलाके में मैंने एक अजीब चीज देखी थी। किसी भी स्त्री या पुरुष की उम्र कितनी भी हो, खासकर स्त्रियों के सारे – के – सारे बाल काले रहते थे। मानो शरीर पर भले ही उम्र का असर होता हो लेकिन सिर के बाल कालातीत थे, उनपर समय बीतने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और वे काले – के – काले ही रहते थे।
इसतरह उस आदिवासी महिला की सब्जी की टोकरी के तरफ मैं स्वयं ही खींचा गया। इस खींचाव का मुझे पता नहीं और न ही मैं इसका कोई नाम देना चाहता हूँ।
मैंने पूछा भी था, “सब्जियों के भाव क्या है?”
वह किसी तरह हिंदी बोल पाती थी. उसने कहा था, “कुड़ी टका।” मैं समझ गया, कुड़ी टका यानी 20 रुपये किलो।
मैं हरी – हरी सब्जियां छांटकर अलग करता गया। छांटी हुई सब्जियों को वह बच्चा ही तराजू में रखता गया। करीब दो किलो जब हो गए तो मैंने ही उसे तौलने को कहा। उसने तराजू उठाई और कुछ झुकाते हुए तौलकर मेरे झोले में डाल दी। मैंने झोले में फिर सब्जियों को चेक किया। मुझे लगा कि एक पीस सब्जी (सब्जी नेनुआ की थी, जिसे दिल्ली में तोरी भी कहा जाता है ) थोड़ी टेढ़ी और कीड़ा खाई हुई जैसी लगी। मैंने उस पीस को उठाकर वापस टोकरी में रख दिया। उसके बदले गलती – से या जानबूझकर दूसरा पीस उठाकर रखने लगा। यह पीस उससे थोड़ा बड़ा था।
मैंने जब उसे रख लिया तो वह महिला अपनी भाषा में बार – बार कुछ – कुछ बोले जा रही थी। उसका मतलब मैं पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। उसके कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े तो मेरी अंदरुनी अहम् की परतें झनझना उठीं. सिर्फ एक शब्द मेरी समझ में आया। “विवेक”
जैसे वह कह रही हो, “आपका विवेक नहीं है कि आप एक छोटे पीस के बदले बड़ा पीस उठाकर रख रहे हो।”
जब मैंने बच्चे से पूछा तो वह भी ठीकसे समझा नहीं सका। लेकिन मैंने जो कुछ समझा बिल्कुल सही समझा. उस महिला ने मेरी अहम् को झकझोर दिया था। हम पढ़े – लिखे लोग दूसरे को अनपढ़, गंवार समझकर, छोटे – छोटे धोखे देकर, अपने को बहुत चालाक समझने लगते हैं। लेकिन दूसरा इतना भी बेवकूफ नहीं होता जितना हम समझते हैं।
मैंने सब्जी का वह पीस उठकर वापस उसकी टोकरी में रख दिया, मानो मैं अपनी भूल सुधारने की कोशिश कर रहा था। परन्तु वह महिला वही पीस वापस मेंरे झोले में रखकर कुछ और बोली जिसका मतलब शायद यही होगा, “आगे से अपना विवेक ठीक रखो, बाबू, दूसरों को बेवकूफ समझने की कोशिश में अपने को बहुत चालाक मानकर ऊँचे मान – सम्मान के अधिकारी मत समझने लगो।”
मेरा विवेक जाग उठा था, मेरा अहं ढह रहा था … लगातार ढहकर गिर रहा था … गिरकर बिखर रहा था … मानो सामने के पहाड़ से झरने के प्रवाह में छोटे – छोटे टूटे चट्टानों के अंश प्रवाह के बहाव में बहा लिए जा रहे हों।
*****
– ब्रजेंद्र नाथ मिश्र
तिथि : 22-07-2015.
बंगलुरु