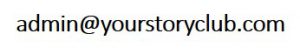ठोस पहिया (Strong Wheel) : This Hindi social story describes a farmer and his family’s struggle to live life & face many crisis during industrialization of independent India.

Hindi Story – Strong Wheel
Photo credit: ganyaman401 from morguefile.com
ऊबड़-खाबड़ स्थल और घिसा-पिटा पहिया, जो मार्ग की सुव्यवस्था न होने के कारण थोड़े समय में ही ऐसी दीन दशा को प्राप्त हो चुका था कि गाड़ी किसी प्रकार घिसटे तो घिसटे, अब सुचारू रूप से चलना उसके लिये सम्भव नहीं प्रतीत होता था। पहिये के जोड़-जोड़ से और चूल-चूल से ऐसी दारुण ध्वनि निकल रही थी मानो कोई सजीव प्राणी हो जिसकी हड्डी-हड्डी चटक रही हो, और वो पीड़ा से चीत्कार कर रहा हो।
वैसे गाड़ी को बने तो अधिक समय नहीं हुआ था, और धनुआ को तो ऐसे लगता जैसे कल की बात हो जब उसने कलुए तरखाण से प्राय: घर का सब कुछ बेच कर यह गाड़ी बनवाई थी। वो उसके पास पहरों बैठा रहता और गाड़ी को बनते देखता रहता। उसने आँखों में बहुत मधुर स्वप्न संजो रखे थे जिनसे उसका मन आनन्द विभोर हो उठता।
धनराज – यानि धनुआ औसत दर्जे का किसान था जिसके पास आधे (पट्टे) की मिलाकर कुल छ: बीघे खेती थी जिससे वो दो एक मज़दूरों की सहायता से बुआई, कटाई कर अच्छा खासा अनाज बीन लेता था जो उसके परिवार की साल भर की ज़रूरत के लिये काफ़ी हो जाता। बाकी समय वो बाप-दादा का मिट्टी के बर्तन बनाने का धन्धा करता था। थोड़ी असुविधा थी तो केवल तैयार माल को मंडी तक ले जाने की। सो अब उसने इसका भी प्रबन्ध कर लिया था। खेत जोतने के लिये घर में बैलों की जोड़ी तो थी ही, वही गाड़ी के आगे जोतने के भी काम आ गई। बैलों के गले में घन्टियों की माला डालकर गाड़ी को सुबह से शाम तक उड़ाये-उड़ाये फिरता जैसे पृथ्वी पर नहीं, आकाश में विचर रहा हो। लगभग उन्हीं दिनों गौरी ब्याह कर आई थी। घर आंगन में पाजेब की झंकार और खेतों में बैलों के गले बंधी घन्टियों की खनक। धनराज को लगता जैसे उसका सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही संगीतमय हो उठा हो।
मार्ग की असुविधायें तो ख़ैर तब भी थीं, जैसे खेतों में आते-जाते गाड़ी का पहिया धम से किसी गड्ढे में जा पड़ता, परन्तु अगले ही पल अपने ही वेग से बाहर भी निकल आता। हां कई बार तो ऐसा भी होता जब उसको दूसरों की सहायता लेने पर बाध्य होना पड़ता। परन्तु सहज ही गाड़ी राह पर लग जाती। यह कोई चिन्ताजनक बात भी नहीं थी। सोचा जाये तो भगवान के अतिरिक्त ऐसा भरा पूरा है ही कौन, जिसे कभी किसी की आवश्यकता न पड़ी हो!
कहने को तो गृहस्थ की गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल सकती, परन्तु देखने में आया है कि गाड़ियां, दो अथवा चार, और विशेष प्रयोजन के लिये तो चार से भी अधिक पहियों की होती हैं। इसलिये यह मुहावरा परस्पर सामाजिक सहयोग का द्योतक हो तो हो, गृहस्थ की गाड़ी से मेल नहीं खाता। हां, गृहस्थ की तुलना एक पहिये से ज़रूर की जा सकती है। जैसे एक पहिया कई एक तीलियों के आधार पर अपनी धुरी से जुड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार, एक पुरुष कई एक आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अथवा शारीरिक बन्धनों से अपनी स्त्री से जुड़ा होता है। यही गोल पहिया हमारी सभ्यता का आधार रहा है।
वैसे तो हर पहिया मार्ग पर चलते-चलते यथाशक्ति बाहरी आघातों से अपनी धुरी को बचाने का भरसक प्रयत्न करता है, चाहे उस चेष्टा में वो स्वयं छलनी-छलनी ही क्यों न हो जाये। वो धुरी पर आंच नहीं आने देता। परन्तु इसकी भी तो एक सीमा है! यह निर्भर करता है, मार्ग की सुव्यवस्था अथवा उसकी क्षमता पर कि वो कब तक अपने प्रयास में सफल हो पाता है।
आधुनिक समाज की आर्थिक विषमताओं के गड्ढे और भ्रष्टाचार की कांटेदार झाड़ियां हर छोटे बड़े पहिये को हलकान किये देती हैं। कोई माने या न माने, पर जब तक मार्ग दुर्गम रहेंगे, और उनको समतल रखने का प्रयास नहीं किया जायेगा, धुरी और पहियों के सम्बन्ध बनाये रखना कठिन हो जायेगा।
अतीत में जब मार्ग सुगम नहीं थे, पहिये ठोस भी हुआ करते थे। जब तक धुरी फैल कर अथवा पहिया सिकुड़कर एक गोल आकार नहीं ले लेता, यात्रा प्राय: असम्भव ही होती है। ऐसे पहिये चलते तो रहे ही हैं, परन्तु बड़ी धीमी गति से।
आज के युग में गति पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस कारण धुरी और पहिये के परस्पर सम्बन्धों का संतुलन बनाये रखने की सामाजिक समस्या है। प्रगति के लिये मार्ग तथा उनकी सुव्यवस्था होना एक अटल आवश्यकता है जिसकी अवहेलना करना प्राय: मूर्खता ही होगी।
इस देश में जब सत्ता दूसरों के हाथ थी, अथवा उनके हाथ थी जिन्हें अपने अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता था, मार्ग निर्माण तथा उसकी सुव्यवस्था की अवहेलना ही होती रही। परन्तु तब हम पराधीन थे। हालांकि दासता के उस दौर में भी पहिये भारी भरकम तो होते थे, मगर होते ठोस और मज़बूत जिनकी गति धीमी तो रहती थी, परन्तु चलते ख़ूब थे।
ख़ैर, धनराज के गृहस्थ जीवन की गाड़ी कई एक कठिनाईयों के होते भी मज़े में चल रही थी। उसे गर्व था अपनी गाड़ी के मज़बूत पहियों पर जो कच्चे-पक्के में, कीचड़-मिट्टी से लथपथ, छोटे-मोटे पत्थरों से सर फोड़ते, रास्ते की झाड़-झंखाड़ को अपने नीचे रौंदते नि:धड़क निकल जाते। और वो उनके सहारे चल रहा था, प्रगति की धीमी गति के साथ।
युग पलटा। भारत स्वतन्त्र हुआ और पहली आवश्यकता जो देश निर्माताओं के समक्ष आयी, वो थी, भूखी जनता को पेट भर अनाज पहुँचाने की। इसलिये इस कृषिप्रधान देश को कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये साधन जुटाये गये और प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई जिसके अन्तर्गत कई एक सिंचाई प्रॉजेक्ट शुरू किये गये और आस बंध गई कि दिनों में ही देश का कायाकल्प हो जायेगा। और ऐसा हुआ भी। योजना के पूरे होते-होते प्रति व्यक्ति आय में दस प्रतिशत की वृद्धि हुई। आवश्यकता तो यही थी कि गांव-गांव को ख़ुशहाल बनाने के लिये ऐसी एक और योजना पर ज़ोर दिया जाये। परन्तु दुर्भाग्यवश यह सब कुछेक हितों के अनुकूल नहीं बैठा।
औद्यौगिक एकाधिपत्य, जिसके लिये कई-एक घरानों ने, जो ब्रिटिश साम्राज्य से क्षुब्ध थे, स्वतंत्रता संग्राम में योजनाबद्ध पूंजी लगा रखी थी, अब और प्रतीक्षा नहीं कर पाये और शीघ्रातिशीघ्र लाभ उठाने के लिये लालायित हो उठे। प्राथमिकतायें बदल दी गईं और भूखे-नंगे किसानों की नीरस कहानी अधूरी छोड़कर भारत को पैरिस बनाने की कहानी शुरू हो गई। तदानुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र से हटकर औद्यौगिक दिशा में चल निकली। बापू का चरखा, जो ग्राम-ग्राम की आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, अब जनसाधारण के पेट भरने का साधन न होकर एक मशीन में परिवर्तित हो गया, जिसे प्रदर्शनियों में एक अनुपम कल के रूप में, नमूने के तौर पर रखा जाने लगा और विशेषकर उसकी पूजा होने लगी जैसे गांधीजी की दूसरी स्मृति-वस्तुओं की। अब इसके कई-एक नये से नये रूप नज़र आने लगे जो चरखा कम, मशीनें अधिक लगते थे।
यह भारत में कलयुग का प्रवेश था।
विद्युत उत्पादन, जो कृषि योजनाओं से जुड़ा हुआ था, पर्याप्त मात्रा में न हो पाने के कारण कोयले पर आधारित हो गया जिसके कारण कोयले की मांग बढ़ गई और ऊँची कीमतों पर प्राप्त किये गये कोयले से सभी वस्तुओं का मंहगा हो जाना स्वाभाविक ही था। हर वस्तु ने तेज़ी पकड़ ली और एक दुष्चक्र गति पकड़ने लगा।
आयात पर रोक लगा दी गई और बड़े बड़े बोर्ड लग गये,”देशभक्त बनिये और देश में बनी वस्तुओं को प्रयोग में लाईये”। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लिये – जहां दूर-दूर तक खेतियाँ लहराया करती थीं – अब मिलों और कारखानों की चिमनियाँ भरपूर धुआँ छोड़तीं नज़र आने लगीं। अब किसी को अनाज की सुध नहीं थी। धड़ाधड़ खेत बिकने लगे। प्राय: पूरे देश में औद्यौगिक क्षेत्रों का निर्माण होने लगा और उनके आस-पास अनाधिकृत बस्तियां बनने लगीं। गांव ख़ाली हो गये और शहरों में भीड़ बढ़ गई। किसान को ग्राहक चाहिये था, जिसकी प्रतीक्षा में खेती की ओर से उसका ध्यान हट गया। दूर दूर तक वीरानी छा गई।
कारखाने बनाने के लिये इमारती सामान की मांग बढ़ने से सीमेंट मार्किट से ग़ायब हो गया तथा ब्लैक में बिकने लगा। सस्ते तथा बेकार माल का उत्पादन बढ़ गया। उपभोक्ता दुखी था कि अच्छे ख़ासे पैसे देने पर भी उत्पादन का स्तर नीचे ही नीचे क्यों जा रहा है! उपभोक्ता संरक्षण के नियम बनाये गये ताकि किसी प्रकार जनता का मुंह बन्द किया जा सके। मानक संस्था की बुनियाद पड़ी। अफ़सरशाही का बोलबाला था, उल्टी सीधी मोहरें लगने लगीं। आम भाषा में ’माल टिकाओ, मिट्टी बेचो’। मानवता अपने नंगेपन पर उतर आई।
दिन प्रतिदिन बढ़ते उद्योगों के लिये मशीनों का आयात आवश्यक था। उसकी पूर्ति के लिये विदेशी मुद्रा जुटाना ज़रूरी था। इसके लिये आलू-टमाटर का निर्यात होने लगा। जो फल-सब्ज़ियाँ ग़रीबों को ठीक दामों मौसम में खाने को मिल जाती थीं, अब ’कोल्ड स्टोरेजों’ में पहुँच गईं। उद्योगपति दिन-प्रतिदिन मोटे होते गये। अफ़सरशाही तथा राजसत्ता को मुट्ठी में करके निर्यात का लाभ उठाने के लिये राजकीय आर्थिक संरक्षण दिया जाने लगा जिससे रही सही कसर भी पूरी हो गई।
होटल, क्लब, जुएखाने और जूस की दुकानों से बाज़ार भर गये। विदेशी कारों और इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की होड़ लग गई। यहां विदेश का सब कुछ मिल सकता था – पर खुले बाज़ार में नहीं। देशभक्ति केवल जनसाधारण के लिये ही रह गई जो बापू का चरखा पकड़कर सर पीटते।
उनकी महफ़िल आईनाख़ाना तो थी लेकिन नदीम ।
सारे आईने सलामत थे, मेरे दिल के सिवा ।।
दूसरी पंचवर्षीय योजना ने तो बेड़ा ही ग़रक करके रख दिया। जो उपलब्धियाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई थीं, सब मिट्टी में मिल गईं। लेने के देने पड़ गये। योजना समाप्त होते-होते देश की अर्थव्यवस्था भी समाप्त हो गई। नेहरूजी के आँख मूंदते ही टूटकर अकाल पड़ा। जनता दाने-दाने को मोहताज हो गई। विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ा। पी. एल. 480 के अंतर्गत अमरीका से अनाज अनुदान के रूप में स्वीकार करना पड़ा। परन्तु वितरण केवल शहरों तक ही सीमित रहा। देश के लिये अनाज जुटाने वाला किसान दाने-दाने को तरस गया। इस रेले में कौन बचा, कौन मरा, किसी को कुछ ध्यान नहीं।
गांव की मिट्टी चिकनी थी। इस कारण देखते देखते आस-पास कई पॉट्रीज़ खुल गईं। पहले पहल तो लगा, धनराज के दिन फिर गये क्योंकि पॉट्रीज़ का माल लादने पर उसे नकद पैसे मिलने लगे थे। कुछ तो मंहगाई के कारण, कुछ शहरी वस्तुओं की सहज उपलब्धता के कारण, घर का ख़र्च बढ़ गया था। परन्तु धीरे-धीरे आमदनी घटती जा रही थी। पॉट्रीज़ में बने सुन्दर तथा चमकदार बर्तनों के मुकाबले उसके बनाये, बेढब, काले कलूटे बर्तनों को कौन पूछता! अब तो गांव वालों को पॉट्रीज़ का रिजैक्ट माल इतना सस्ते में मिलने लगा कि सिवाय कुछेक घरों के, जिनकी ठंडे जल के लिये उपयोगिता कम नहीं हुई थी, बाकी माल किसी भी भाव नहीं बिकता। देखते ही देखते उसका आवा ही ठंडा पड़ गया।
माया तेरे तीन नाम, परसू, परसा, परसराम ।
अब धनराज, धनुआ के नाम से जाना जाने लगा – धनुआ गाड़ीवाला। यहां तक भी ठीक ही था, परन्तु शहर से टायरों वाली गाड़ियों की भरमार हो गई और उसका यह धन्धा भी चौपट होता नज़र आया। हवा से फूले, रबर के ये टायर उद्योगपतियों के अधिक काम के थे। तैयार माल की सुरक्षा के अतिरिक्त समय की भी बचत होती थी। इस कारण धनुआ को अब काम कम ही मिलता। और यदि मिलता भी तो बहुत कम मज़दूरी पर जिससे घर में प्राय: रोज़ ही झगड़ा होने लगा और वो समय-असमय दारू के ठेके पर देखा जाने लगा, जिससे पहिये और धुरी के सन्तुलन को बनाये रखना कठिन सा हो गया।
गति का युग आ गया था और प्रगतिशील समाज के सामने तो ये समस्यायें आनी ही थीं ! पहिये की अपेक्षा धुरी का महत्व बढ़ गया था। अब वो पहिये पर सीधे निर्धारित न होकर कई एक फिसलने वाले रोलरों अथवा बॉल-बीयरिंग के द्वारा सम्बन्धित थी। ग्रीज़ का तो महत्व था ही। यह भी एक सामाजिक विडम्बना थी जो हमारे पुराने विचारों के अनुरूप नहीं बैठी।
मार्ग की धूल-मिट्टी चाटना तो अब भी पहिये का भाग्य था। परन्तु अब, आधुनिक पहियों में पहले की अपेक्षा मज़बूती और सहनशीलता नहीं थी। धुरी को गति प्रदान करने के लिये उनको नर्म-नर्म फूले हुए टायर पहनने पड़ते थे। इससे चोट तो कम लगती, परन्तु आत्मनिर्भरता प्राय: नष्ट हो गई थी। कहां तो वो झाड़-झंखाड़ को पैरों से रौंदने में सक्षम थे, और कहां अब एक छोटे से कांटे की चुभन भी सहन नहीं कर सकते थे। जैसे ही कोई छोटा-मोटा कांटा लगा, एकदम से हवा सरक गई। परन्तु यह समस्या उद्योगपतियों की नहीं थी। धुरियाँ अब स्वतंत्र रूप से कई एक परिधियों में घूमने लगी थीं। जहां ग्रीज़ द्वारा फिसलाने की क्षमता अधिक होती, वहां धुरी अधिक समय तक टिकती।
पता नहीं क्यों, ये हल्के-फुल्के टायरों वाले पहिये मन को बहुत भाते थे। गोल-मटोल चमकदार पहिये, जिनपर चढ़े काले-काले टायर, ऐसा लगता, जैसे किसी साम्राज्यवादी पल्टन के सिपाही हों, और चुस्त चौबन्द वर्दी पहने, काले जूतों से लैस, एड़ियां बजाकर साहब लोगों को सलामी दागने के लिये तैयार खड़े हों।
सम्भवत: वो जीवन की एकरसता से ऊब गई थी। सदियों से दबे उसके नारी सुलभ जीवन में कुछ नया करने की महत्वाकांक्षा जाग उठी। बिना कुछ सोचे-विचारे, जाने-बूझे, कि वे अपरिचित रास्ते उसके खेत-खलिहान को नहीं, बल्कि कहीं दूर वीरानों में निकल जाते हैं, उसने धनुआ से ज़मीन बेचकर पहियों में टायर लगवाने की बात की और दबी ज़ुबान में गांव की दूसरी औरतों के समान पॉट्री में काम करने की अनुमति मांगी। गांव के बड़े-बूढ़े बहू-बेटियों के पॉट्रियों में काम करने के विरुद्ध थे। परन्तु मंहगाई से दबा धनराज, थोड़ी अतिरिक्त आय की लालसा में उसे काम से नहीं रोक सका।
जहां तक पहियों में टायर चढ़ाने का प्रश्न था, यह उसके बूते की बात नहीं थी। एक तो ज़मीन का मोह – जो पहले ही गिरवी पड़ी थी – और दूसरे पहियों की खस्ता हालत, उसके लिये टायरों की बात सोचना ही अटपटा सा लगा। परन्तु वो मन ही मन यह भी भली प्रकार जानता था कि समय के अनुसार हल्के-फुल्के टायरों की आवश्यकता तो है। उसे इसका भी ज्ञान था कि नाज़ुक-नाज़ुक तीलियों के सहारे पहिये टायरों को ओढ़ने की कितनी क्षमता रखते हैं। सुगमता तो धुरी को अवश्य होगी, जो सरलता से घूम सकेगी, और रास्ते के कांटों की आशंका के रहते भी कितनी सरलता से घूमेगी! परन्तु ’मरता क्या न करता’, ज़मीन भी तो गिरवी पड़ी थी! उसे बेचने का मन बनाते बनाते, वो प्रगति की दौड़ में बहुत पीछे रह गया था। उसकी जानकारी अथवा अनुमति के बिना लोगों ने उसकी ज़मीन को खोद-खोद कर गड्ढा बना दिया था। जिस कारण उसके पैसे अब इतने कम मिलने लगे थे कि वो साहूकार का कर्ज़ ब्याज सहित चुकाकर टायरों के लिये पैसे नहीं बचा सकता था। चार पैसे बचते तो झुग्गियाँ बनवाकर मज़दूरों को किराये पर उठा देता। परन्तु इस से कब्ज़ा हाथ से निकल जाने का डर था। इस कारण निराशावश उलझन में वो सोच में डूबा रहता, अथवा दारू में। गौरी मज़दूरी करके चार पैसे ले आती जिस से दाल-भात की व्यवस्था हो जाती। और धनुआ दारू के लिये खेत की मिट्टी – जिसपर वो भरपूर खेती किया करता था – खोदकर, अपनी बैलगाड़ी भर कर पॉट्रियों में बेच आता।
गौरी को काम पर आते-जाते कई-एक मज़दूरों ने घूरना शुरू कर दिया था। काम की तलाश में आये उन मज़दूरों को – जो अपने परिवारों से बिछड़कर गांव में आये थे – अब, जब खाने को भरपेट रोटी मिलने लगी तो उन्हें मस्ती सूझी। अब रोज़-रोज़ घर जाने से तो रहे, वहीं पर कामगार स्त्रियों पर रीझ जाते थे। चाहे वे उनसे बड़ी उम्र की ही क्यों न हों। यह पशुवृत्ति की दूसरी मांग थी। औद्यौगीकरण की यह भी एक समस्या है कि जिस आवारागर्दी से कम से कम गांव अछूते थे, अब दारू, जुए, और व्यभिचार के अड्डे बन गये थे। कोई कहां तक बच पाता! एक ही स्थान पर तो काम करना था!
चार बर्तन होंगे तो टकरायेंगे भी अवश्य। और इस खंकार को सुनने के लिये लोग तो सदा ही लालायित रहते हैं। पहिया चरमरा रहा था। परन्तु धुरी में अभी काम चलाऊ शक्ति थी। थोड़ी ग्रीज़ मिलने पर चल निकली। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। पर धनुआ, जिसकी कमर अधिक परिश्रम, और दारू की वजह से पहले ही टूट चुकी थी, बस सुनता रहता, परन्तु गौरी को कुछ न कह पाता, मन ही मन कुढ़ता, निराशा से घिरा, फिर दारू के अड्डे पर लौट आता। अब यही उसका जीवन हो गया था। परन्तु यह सब कब तक चलता! एक दिन, कड़कती दोपहर में पॉट्री पर काम करते हुए गौरी को उसके निधन का समाचार मिला। स्वाभाविक एक झटका तो अवश्य लगा, और दुनियादारी निबाहने के लिये सोग भी मनाया, परन्तु उसके मन को विशेष आघात नहीं पहुँचा था। क्योंकि सम्बन्ध तो प्राय: कब के विच्छेद हो चुके थे – सिवाय दो बच्चों के, जिन्हें धनुआ से डर सा लगने लगा था, जो दारू के नशे में धुत, गिरता पड़ता, देर रात घर को लौटता और आते ही गौरी को किसी न किसी बहाने पीटने लगता, अथवा बाहरी दालान में चित हो जाता। इन अबोध बच्चों को दुख तो क्या होता, विपरीत इसके, उन्होंने सुख की सांस ली।
ज़्यादा समय नहीं बीता कि मुश्टंडे, जो अभी तक पॉट्री तक सीमित थे, अब घर तक पहुँचने लगे। अब गौरी पर उनकी पकड़ अधिक मज़बूत हो गई। कभी कोई मलाई, कभी कोई मिठाई का दोना लेकर घर पर आ धमकता और बच्चों को बहला फुसलाकर खेलने को भेज देता, और स्वयं गौरी को नोचने खसोटने लगता।
उनमें विशेष रूप से पॉट्री का एक गेटमैन गिरिजाप्रसाद तिवारी था जो गौरी को बहुत भाता था। चुस्त कोट-पतलून पहनकर फ़जलबूट पहने, वो उसे किसी रियासत के राजकुमार से कम नहीं लगता था। आयु भी उसकी अधिक नहीं थी। केवल बाईस वर्ष, जिस आयु में – सुनते हैं – व्यक्ति गधा-पचीसी भोग रहा होता है। वो ’काम का न काज का’ दुलत्तियाँ अधिक झाड़ता था। फिर भी गौरी उसे बहुत पसंद करती थी। बुद्धि तो प्राय: सभी की इस उम्र तक कम ही विकसित होती है, एक दिन आया कि वो घर का सदस्य ही बन गया, और किसी को कहे सुने बग़ैर, घर के मालिक का स्थान ले लिया। और जात बिरादरी ने भी यह मान लिया कि इधर-उधर मुंह मारने के बजाय ’गाय खूंटे पर तो लगी’! वो अब जो कमा कर लाता, गौरी को सौंप देता। समय अच्छा कटने लगा।
गौरी को इसका ज्ञान नहीं था कि ज़मीन गिरवी पड़ी है। चूंकि चार पैसे इकट्ठे हो गये थे, इसलिये उसने ज़मीन पर चार झोंपड़े बनवाने का प्रबंध किया। परन्तु साहूकार ने झट दारोगा को साथ लेकर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और झुग्गियों का काम रुकवा दिया। शन्नो, जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, साहूकार के इस व्यवहार पर खीझ उठी। उसकी अल्पबुद्धि के अनुसार, साहूकार उनकी ज़मीन छीन रहा था। इस कारण उसके मन में उसके प्रति विद्रोह की भावना जाग उठी। और यही भाव उसने अपने छोटे भाई दीपू के मन में भी जगा दिया जो अभी बहुत छोटा था और इस सबके लिये तैयार नहीं था। घृणा उसके अंतर्मन में घर कर गई और बदले की आग भड़कने लगी।
इस घटना को भी अब सात वर्ष हो गये हैं। शन्नो अब सोलहवें-सत्रहवें में प्रवेश कर चुकी है और दीपू बारह का है। भरपेट खाने को मिल जाता है। वैसे भी सुनने में आया है कि वीरानों में खिले फूल कुछ अधिक ही सुन्दर दीख पड़ते हैं – शन्नो भी बला की हसीन थी, और गिरिजाप्रसाद अपने भरपूर यौवन पर था। एक ही घर में रहते थे, किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं थी, आखिर अग्नि के सामने घी टिक नहीं पाया और जल्दी ही पिघल गया। बाप समान गिरिजाप्रसाद ने इस अवसर का अनुचित लाभ उठाया और जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो एक दिन – जब गौरी काम पर गई हुई थी – शन्नो को लेकर फ़रार हो गया। बहुत थू-थू हुई, परन्तु गौरी कह क्या सकती थी! मन मारकर लोगों से झूठ-मूठ कहती फिरती कि उसने अपने हाथों दोनों का ब्याह किया है। परन्तु लोग कब मानने वाले थे! अब गांव भर में – और इधर-उधर के गांवों में भी – उसकी चर्चा होने लगी थी। आते-जाते मुश्टंडे फब्तियां कसते, और साथ की कामगार स्त्रियां तो जैसे उसे अछूत मानने लगी थीं। कोई भी उसके पास बैठकर सांत्वना के दो शब्द कहने को तैयार नहीं था। सिवाय दीपू के, जो न तो पढ़ा लिखा था और न अभी मज़दूरी लायक। काम ढूंढने निकलता तो वही जली-कटी सुनने को मिलती। सारा-सारा दिन आवारा छोकरों के साथ जुआ खेलता और बीड़ी के लम्बे लम्बे कश लगाता। घर आता तो दुखी माँ को बात-बात पर खाने को दौड़ता ।
अब गौरी को महसूस हो रहा था कि क्यों उसने बिना सोचे समझे ग़लत राह चुन ली थी जिसने अब उसके जीवन के इस अंधियारे पक्ष में अकेली राहों पर छोड़ दिया था। अब वो अतीत की चन्द मधुर स्मृतियों के सहारे जीवन व्यतीत करने लगी, परन्तु वो न तो अब आगे बढ़ सकती थी, न ही पीछे जा सकती थी।
यदि गहराई से सोचा जाये तो उसका दोष था भी तो कितना! यही न कि उसे चमचमाते काले टायरों वाले पहिये भा गये थे! परन्तु यह तो कोई विशेष दोष नहीं! जब आँखों के सामने रौशनियाँ जगमगा रही हों तो आँखें तो चौंधियायेंगी ही। यदि जगमगाहट धीरे-धीरे होती तो सम्भवत: आँखें उन्हें देखने की अभ्यस्त हो जातीं। और अब तो वो समय भी शीघ्रातिशीघ्र आने वाला है जब अणुओं के टकराने से रौशनी बहुत तेज़ हो जायेगी। उस समय यदि तुम्हारी आँखें जल उठेंगी तो इसमें अचम्भा किस बात का! दोष आँखों का नहीं, गति का है जिसने इतनी तीव्रता ग्रहण कर ली है कि अब वो किसी को आड़े नहीं आने देगी।
हर तीव्र प्रकाश के बाद अंधेरा तो छा ही जाता है। जब हाथ को हाथ न सूझेगा तो इस अंधेर-युग में जनसाधारण तो डूब ही जायेगा। अब कहने को विशेष रह ही क्या गया है!
शन्नो का आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगा, पर गिरिजाप्रसाद की तृष्णा में कमी नहीं आई। वो इधर-उधर मुंह मारने लगा। परन्तु यह तो समय की पुकार है। दोनों ने अलग-अलग कोठे ढूंढ लिये।
दीपू कुसंगत में पड़ चुका था, और शन्नो के दिये विचारों ने उसके मन में इतनी कटुता भर दी थी कि उसने साथियों के साथ मिलकर साहूकार के यहां डाका डालने की योजना बना डाली। पता नहीं कैसे साहूकार को इसकी पूर्व सूचना मिल गई और वो साथियों के साथ भागते हुए पुलिस की गोली का निशाना बन गया।
सुनते हैं, गौरी अब भी पॉट्रियों के सामने बैठकर, हर आने-जाने वाले के सामने हाथ फैलाती है। वो ख़ुदा की मेहर और नाख़ुदाओं की करम-फ़रमाई से अपने अतीत को भूल ही चुकी है। और…
दोबारा मंज़िले-ख़ूंबार की तरफ़ हैं दवां ।
वो रहनुमा जो कई बार राह भूले हैं ।।
यही हमारी सभ्यता की ’चमक दमक’ है।
समाप्त
लेखक :- जगदीश लूथरा ‘नक्काद’