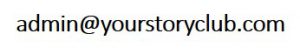लायन्स क्लब – Lions Club (When a writer got invitation for a famous club’s party, he was shocked. He went there to find out the truth and he was surprised again. Read Hindi story)

Hindi Story – Lions Club
Image Source: www.cepolina.com
अपने नाम लायन्स क्लब का मोहरबन्द लिफ़ाफ़ा पाकर मैं चकित रह गया। मेरा अभी तक किसी लायन से सामना नहीं हुआ था। और लायन्स क्लब से तो मेरा जैसे दूर का भी वास्ता नहीं था। फिर अचानक यह दावतनामा मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के नाम! मैं कुछ समझ नहीं पाया। पहला झटका जो मेरे मस्तिष्क को लगा, मैं ज्यों त्यों करके झेल गया। परन्तु जैसे जैसे इसका प्रभाव शरीर के अन्य अंगों पर तथा तंत्रिकाओं पर पड़ा, लगा जैसे सांस तेज़ हो गई हो और हृदयगति रुकने लगी हो। मेरे मस्तिष्क की क्या स्थिति थी मैं बयान नहीं कर सकता। चार सीढ़ियाँ चढ़कर घर के द्वार तक पहुँचना कठिन हो गया। ख़ैर ज्यों त्यों करके अधखुला लिफ़ाफ़ा हाथ में लिये, घर में जा पहुँचा और सामने ही पड़ी चारपाई पर धम से ढह सा गया। चेहरे का रंग उड़ गया होगा अथवा पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और पीलिया गया होगा क्योंकि नज़र पड़ते ही श्रीमती जी दौड़ कर आयीं और रुहांसे स्वर में पूछने लगीं, “क्या हुआ?”
मैंने निर्जीव से हाथों थामा हुआ लिफ़ाफ़ा आगे बढ़ा दिया परन्तु वो निपट गंवार बेचारी क्या जानतीं उस लिफ़ाफ़े का महत्व! घबराकर पल्लू डाल रोने लगीं। तब कहीं जाकर मुझे होश आया और उसे समझाया कि रोने धोने लायक ऐसी कोई बात नहीं है, यह मेरे नाम आया हुआ एक दावतनामा है – अशोका होटल में शाम के डिनर का। तब जाकर उसे धैर्य बंधा।
’लायन्स क्लब के सौजन्य से’- यह वाक्य मैंने कई बार, बस स्टैन्ड पर बस की प्रतीक्षा करते, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ पढ़ा था। इसके अतिरिक्त लायन्स क्लब के बारे में मेरी जानकारी शून्य मात्र थी।
हां, एक बार जब भारत माता अस्पताल में बीमार थी – शायद मैंने इसका उल्लेख अपनी लघु-कथाओं में कहीं किया है – ’लॉयन्स क्लब के सौजन्य से’ फ्रूट्स के कई टोकरे रोगियों में बंटने के लिये आये थे – ऐसा मैंने सुना था – जिनका अधिकांश भाग स्टाफ़ ने अपने स्वास्थ्य-वर्धन के लिये उड़ा लिया था।
परन्तु आज यह कृपा विशेष मुझ पर ही क्यों हुई, मुझे इसका विश्वास नहीं हो रहा था। नाम, पता कई बार जांचा कि कहीं ग़लती से तो डाकिया किसी और का लिफ़ाफ़ा मेरे घर नहीं डाल गया! मगर ऐसा लगता नहीं था। यह भूल थी तो केवल भेजनेवाले की जिसने बिना कुछ सोचे समझे मुझ निहत्थे पर अपना अमोघ बाण चला दिया था। परन्तु वो कौन होगा जो अपने बाप-दादा की कमाई इस बेदर्दी से लुटा रहा है, और वो भी मुझ जैसे फक्कड़ लेखक पर, जिसके अपने सम्पादक ही सोच विचारकर गिरह खोलते हैं!
भेजनेवाले के नाम से तो कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। लिखा था,’साइनो ग्रुप ऑफ इन्डस्ट्रीज़’ के चेयरमैन ’लायन बृजेश्वर दयाल गुप्त’ – यह कोई बहुत बड़ी हस्ती लग रही थी। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल साफ़ था। मैं भूले से भी कभी साइनो इन्डस्ट्रीज़ के सामने से नहीं गुज़रा हूं और मुझे यह तक भी ज्ञात नहीं कि साइनो इन्डस्ट्रीज़ के नाम की कोई संस्था देश में मौजूद है। बिना सोचे समझे शेरों की मांद में मुझे तो निरर्थक बलि चढ़ने के समान लग रहा था। फिर ख़्याल आया कि मेरे किसी लेख से चिढ़कर किसी ने प्रतिशोध की भावना से होटल में बुलाकर अपमानित करने की तो नहीं सोची! परन्तु मैं कब से इतना प्रभावशाली लेखक हो गया कि मुझे नीचा दिखाने के लिये कोई इतना बड़ा आयोजन करने लगा! और फिर मच्छर मारने के लिये तोप दागने की क्या आवश्यकता थी! मैं तो वैसे ही मरा हुआ हूं – आर्थिक, तथा सामाजिक दृष्टि से भी। यह भी विचार आया कि मज़ाक के तौर पर मुझे एप्रिल फ़ूल तो नहीं बनाया जा रहा! परन्तु अभी तो दीवाली भी नहीं आयी। एप्रिल फ़ूल बनाने के लिये कोई क्यों अपना दीवाला निकालने लगा!
यही सब सोचते काफ़ी समय बीत गया। अचानक श्रीमती को दूर की सूझी। बोली, “क्यों न यह दावतनामा और वो भी अशोका होटल का, कुछ पैसे लेकर किसी के हाथ बेच दिया जाये!”
सुझाव जानदार था, परन्तु मेरे जानकारों में अधिकतर मेरे समान पैसे-पैसे को मोहताज व्यक्ति ही थे। कौन इस स्थिति में था कि दावतनामा ख़रीदकर अशोका होटल में डिनर करने जाये! और फिर इसके लिये समय भी कहां था! दावत उसी दिन शाम को ही थी – नौ बजे। मैं निरुत्साह होकर बैठ गया। परन्तु श्रीमतीजी कब मानने वाली थीं! और मानतीं भी कैसे! जीवन में पहली बार तो यह महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ था! कहने लगीं, “आप ही हो आईये न! शायद इस तरह बड़े लोगों में उठने बैठने से भाग्य चमक उठे!”
उनका विचार था कि माँ सरस्वती को मेरी लेखिनी पर दया आ गई थी। कहने लगीं, “अब तो बड़े-बड़े लोग आपको खाने पर बुलाने लगे हैं।”
मन तो नहीं मानता था, परन्तु न मानने की वजह भी नज़र नहीं आ रही थी। और फिर कैरियर का भी सवाल था। वैसे भी मेरी उत्सुक्ता बढ़ गई थी – यह जानने के लिये कि यह महाशय श्री बृजेश्वर दयाल गुप्त हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं! कुछ सोच-विचार के बाद जाने को तैयार हो गया। इसके अतिरक्त -“मुफ्त का माल था, हाथ से छोड़ा न गया।”
परन्तु समस्या एक और भी थी। पहनने लायक कपड़े कहां से लायें! आने जाने की व्यवस्था, बुके वगैरह के लिये भी पैसे और बोलने को चार शब्द – क्योंकि मैं एक लेखक हूं। लिखना तो मेरे लिये कोई समस्या नहीं थी। हालांकि मुझे अवसर की विशेष जानकारी नहीं थी, परन्तु घिसे पिटे शब्द तो मैं कभी भी और कहीं भी कह सकता था। पर जाने आने का ऑटो का भाड़ा भी तो चाहिये था! क्योंकि देर रात को अशोका से मेरे घर आने का कोई साधन नहीं था। बस तो तब तक बन्द हो चुकी होगी! अबकि फिर श्रीमतीजी ही काम आयीं। बोलीं, “मैंने कुछ पैसे घर ख़र्च से बचाकर रख छोड़े हैं। अभी निकालकर लाती हूं। आने जाने के लिये टैक्सी स्कूटर कर लेना। और बुके में लगता ही क्या है, पचास-साठ रूपये! सो वो भी ले लेना।”
रात के समय हल्की सर्दी तो पड़ने लगी थी, परन्तु गर्म कपड़े थोड़ा पैसे के अभाव में ड्राईक्लीनिंग के लिये नहीं निकाले गये थे। एक जोड़ा, जो कुछ साफ़-सुथरा लग रहा था, निकालकर प्रैस करने बैठ गया। अभी समय भी कुछ विशेष नहीं था, नहा-धो कर आवश्यकता से कुछ अधिक ही पहले बन संवर कर तैयार हो गया और आठ बजते-बजते होटल की राह ली। होटल दूर तो काफ़ी था, परन्तु समय भी पर्याप्त होने के कारण मैं पैदल ही चल निकला और नौ बजते-बजते होटल के हॉल में प्रविष्ट हो गया तथा जश्न में शामिल हो गया।
डिनर क्या था, अच्छा-खासा मेला लगा हुआ था। मेरी आशंकायें निरर्थक सिद्ध हुईं क्योंकि मेरी ओर किसी ने आँख उठाकर भी नहीं देखा। दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई कि शायद कोई परिचित निकल आये, परन्तु मेरे लिये सब अपरिचित ही थे। और आपस में ख़ूब हंस बोल रहे थे। मुझे कुछ अटपटा सा लगा और दूर कोने में रखी एक अकेली कुर्सी पर, जिसपर सम्भवत: किसी की नज़र नहीं पड़ी होगी, या किसी ने बैठना पसन्द नहीं किया होगा, हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर जा बैठा और चुस्कियाँ लेने लगा। मेरे समान और भी बहुत सारे लोग हाथ में गिलास थामे घूम रहे थे जिनमें लगता था, कोका कोला तो नहीं, शायद व्हिस्की रही होगी।
कुछ समय बैठने के पश्चात् मुझे लगा कि सभी आगन्तुक एक व्यक्ति-विशेष की ओर जा रहे थे जो बड़ी विनम्रता से अभिवादन कर सबको बैठने का संकेत कर रहा था। शायद यही मेरा मेज़बान लायन बृजेश्वर दयाल गुप्त था। दूरी अधिक थी और डिनर के लिये रौशनी पाश्चात्य सभ्यता के रिवाज़ानुसार थोड़ी मध्यम ही रखी गई थी। मैं उस व्यक्ति को पहचान नहीं सका। मैं सोच ही रहा था कि मैं भी उठ कर उस से हाथ मिलाऊं, कि अचानक साईड पर बने स्टेज की रौशनी में वो नहा सा गया और ऑरकेस्ट्रा का स्वर मध्यम हो गया।
एक सुन्दर और प्रभावशाली महिला मटकती हुई, हाथ में माइक लिये स्टेज पर नमूदार हुई और लगी अवसर-विशेष की गरिमा बघारने। इसके बाद लायन्स क्लब के प्रदेश अधिकारी, जिनका भला सा नाम था – जो अब मुझे याद नहीं आ रहा – उपस्थित सज्जनों को अपना परिचय देते हुए लायन बृजेश्वर दयाल गुप्त को स्टेज पर आने के लिये आमंत्रित करने लगे। स्टेज तो रौशनी से जगमगा ही रहा था, बृजेश्वर दयाल के स्टेज पर कदम रखते ही, मैं अवाक् सा रह गया। अरे यह तो वही बी. डी. गुप्ता था जिसे हम हंसी-मज़ाक में बदबूदार गुप्ता कहते थे! नये सूट में आज दस-बारह साल बाद भी क्या सजीला जवान लग रहा था।
यहां से कहानी फ़्लैशबैक में चली जाती है।
मैं नया-नया दिल्ली आया था और बड़ी कठिनता से यह स्थान – जिसमें मैं अब भी अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रह रहा हूं, और जिसमें केवल दो ही कमरे हैं – पिताजी के एक पूर्व-परिचित के माध्यम से प्राप्त करने में सफ़ल हो गया था। नई-नई नौकरी लगी थी। किराया मेरी हैसियत से कुछ अधिक था और मैं अकेला था, इसलिये किसी को अपने साथ रखने की सोच रहा था कि कुछ किराये में सहूलत मिल जाये। परन्तु अभी तक कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला था।
एक दिन ऑफ़िस से ओवरटाईम करके लौट रहा था कि स्टेशन के पास ही बस-स्टॉप पर एक सज्जन से भेंट हो गई। उस दिन सर्दी कुछ अधिक ही रही होगी, क्योंकि वो अच्छे-खासे कपड़े – गर्म सूट – पहने हुए भी सर्दी से कांप रहा था। पूछने पर पता चला कि वो परदेसी है और अभी-अभी गाड़ी से उतरा है, कि अचानक ज्वर आ जाने के कारण उठने तक की हिम्मत भी खो चुका है। मुझे दया आ गई और उसे रात काटने के लिये पल्ले से स्कूटर के पैसे ख़र्च करके, घर लिवा लाया। दो दिन के पश्चात् उसने अपनी इच्छा प्रकट की और मुझे भी आवश्यकता तो थी ही, दोनों की बात पट गई और बी. डी. गुप्ता, जिसकी विशेष जानकारी प्राप्त करने की मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी, आधा किराया देने पर मेरे साथ रहने को तैयार हो गया। मेरा कमरा कैसा था, उसने भी ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं की, और एक माह का किराया नकद देकर रहने लगा।
मगर यह उसकी पहली और आख़िरी अदायगी थी। क्योंकि अपने-आप उसने मुझे किराया देने की ज़रूरत नहीं समझी और मैंने संकोचवश उस से मांगा नहीं।
मैंने सोचा था कि सामान वो शायद बाद में लायेगा, परन्तु उसके पास लाने को कुछ था ही नहीं। एक सूट था जो उसने एक छोटे से थैले में रखा हुआ था। वो एक सूट पहनता तो दूसरा ड्राईक्लीनिंग के लिये दे आता। मोजे, बनियान तो शायद उसके पास थे ही नहीं। या उसने बदलने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं की। न ही उसके पास बदलने के लिये लुंगी, बिस्तर था। और प्राय: बिस्तर भी मेरा ही इस्तमाल कर रहा था।
उससे हमेशा एक प्रकार की दुर्गन्ध आती रहती थी, जिस कारण मेरे इष्ट-मित्रों में उसकी काफ़ी चर्चा रहने लगी। काम-काज तो मेरी जानकारी के अनुसार कुछ करता नहीं था, परन्तु पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। बावजूद इसके, ढाई-तीन माह जो वो मेरे साथ रहा, मेरा ही तौलिया-साबुन बरतता रहा।
वो रात को देर से लौटता और कमरे में पड़ी चटाई, दरी पर मेरी ही एक चादर और कम्बल ओढ़कर सो जाता। मैं भी ओवरटाईम में व्यस्त रहता, और ज़्यादातर उसको घर से नदारद ही पाता। दो-एक बार दिन में मुलाकात हुई भी। वो ऊँची-ऊँची हांकता। मेरे मित्र कहा करते कि वो कोई बिगड़ा दिल रईस है और मेरी ख़ातिर उसकी उल्टी-सीधी सुन लेते। हालाँकि पीठ पीछे जब भी उसका ज़िक्र आता, बदबूदार गुप्ता कहकर स्मरण करते। मुझे एक बार भी यह ख़्याल नहीं आया कि वो वास्तव में कितना धनाढ्य व्यक्ति होगा। अपनी व्यस्तता के कारण मैंने भी ज़्यादा जानने का यत्न नहीं किया कि वो कौन है और दिल्ली में कहां से आया है। और उसने भी अपने बारे में विशेष कुछ नहीं बताया। हां, इतना अवश्य हुआ कि एक दिन मुझे ऑफ़िस में आकर मिला और बताया कि उसके पिता बीमार हैं, और वो तुरन्त हिसार – अपने घर – लौटना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन उसके पास किराये लायक पैसे नहीं हैं। मैंने अवसर की गम्भीरता पहचानते हुए हिसाब-किताब करना ठीक नहीं समझा। उल्टा उसके मांगने पर तीस रूपये उधार दे दिये। उसने धन्यवाद देते हुए इस वायदे के साथ स्वीकार कर लिये कि जाते ही भेज देगा और इस हेतु अपनी डायरी निकालकर मेरे सामने मेरा पूरा नाम और पता भी नोट कर लिया।
मेरे पैसे तो ख़ैर न आने थे न आये, मगर आज अचानक अनहोनी घट गई। मेरे नाम यह दावतनामा भेज कर उसने हिसाब चुकता कर लिया। फिर भी मैंने मन ही मन में उसकी सराहना की कि कितना उदार व्यक्ति है! अपनी पोज़ीशन का ध्यान न करते हुये मुझ जैसे निर्धन को याद किया है। इसके लिये मुझे उसका आभारी होना चाहिये। यही सब जताने के लिये मैं लालायित हो उठा कि उसको मिलकर अपनी कृतज्ञता जताऊँ।
परन्तु यह मेरी भूल थी। वास्तव में ऐसा नहीं था। दावतनामा उसकी जानकारी में न होते हुए ही मुझ तक पहुँचा था। इसका ठोस प्रमाण तो नहीं था, परन्तु यह सच था कि बी. डी. गुप्त वास्तव में एक धनी परिवार का एकमात्र सुपुत्र था, और अपने बाप से नाराज़ होकर एकाध सूट लिये, कुछ पैसे बटोरता हुआ दिल्ली भाग आया था। कुछ समय धक्के खाने के बाद, जब जेब ख़ाली हो गई तो मुझसे तीस रूपये उधार लेकर वापिस लौट गया था। तब उसने वायदा किया था कि वो जाते ही मुझे वो पैसे भेज देगा, और इसके लिये अपनी डायरी में मेरा नाम और पता भी नोट कर लिया था। पैसे तो उसने न भेजने थे, न भेजे, पर बाप के मरने के बाद, जब वो कारोबार को सम्हालने वाला एकमात्र व्यक्ति बना तो उसके सेक्रेट्रियों ने शायद ग़लती से मेरा वही नाम और पता उसकी पुरानी डायरी से नई डायरी में स्थानान्तर कर दिया होगा। यह निमंत्रणपत्र भी उसी स्थानान्तरण का एक हिस्सा रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है।
लायन बृजेश्वर दयाल गुप्त, प्रदेश अधिकारी के कहने पर स्टेज पर आये और हाथ में लिखे कागज़ के बावजूद, अटक-अटक कर, उपस्थित सज्जनों को सम्बोधित करने लगे और झुक-झुक कर धन्यवाद देने लगे, जिन्होंने अति कृपा करते हुए उनके बुलाने पर मुफ़्त का माल खाने का कष्ट किया था। मुहावरे के अनुसार -’झुकते हैं सखी वक़्ते करम और ज़ियादा’। इसके मुताबिक श्री गुप्त के मुंह से शब्द तो कम ही निकल रहे थे, परन्तु तालियों की गड़गड़ाहट में वे थोड़ा-बहुत जो कह पाये, वो भी मेरे कानों में नहीं पड़ा। अब बहुत सारे सज्जन स्टेज पर जा-जा कर उन्हें मुबारक दे रहे थे – स्थानीय अध्यक्ष नियुक्त होने के लिये।
मैं भी उठा और आगे बढ़कर, मुबारक देते हुये, अपना हाथ आगे कर दिया। मगर उसके तो तेवर ही बदले हुए थे। अपना हाथ खींचकर बड़े बेतुके अंदाज़ में बोला, “आप यहां क्या कर रहे हैं? अपने पैसे वसूल करने आये हैं?” और पर्स निकालने के लिये अपनी जेब की ओर हाथ बढ़ाया। इससे पूर्व कि मैं कुछ उत्तर देता, उसके निजी सचिव ने, जो मेरी फटेहाली से जान चुका था कि मेरी उपस्थिति रुचिकर नहीं है, झट से मेरा हाथ थामते हुए कहा, “अरे आईये नेताजी।” और मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोला, “क्षमा करना, गुप्ताजी ने आज कुछ ज़्यादा ही चढ़ा रखी है।” और फिर वो मुझे खींचते हुए हॉल में खाने की टेबलों के पास ले गया। बैरे से एक प्लेट पकड़कर मुझे थमाते हुए क्षमा याचना करता भीड़ में कहीं लीन हो गया। उसे क्या मालूम था कि उसका यह सभ्य दीखने वाला बॉस कितना नीच है, जो दस-बारह साल के उधार को ब्याज-दर-ब्याज चुकाने के लिये आज मुझे अपमानित कर रहा है। हालाँकि वो आज भी मेरा तीस रूपये का कर्ज़दार है। मुझे बताने में लज्जा अवश्य आ रही है कि अच्छे-अच्छे व्यंजनों से भरी हुई थाली तो मेरे हाथ में थी, परन्तु हलक से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा। मैं अपने सरल स्वभाव पर दुखी, यहां आकर पछता रहा था।
मुझे याद पड़ता है, किसी लेखक ने लिखा था कि, ‘शहर एक घना जंगल है’। उसने यह किस संदर्भ में लिखा था, मैं यहां नहीं दोहराऊंगा क्योंकि यह शब्द एक आतंकवादी के हैं। परन्तु इस सच्चाई को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि वास्तव में शहर जंगल हों या नहीं, यहां पर नियम जंगल का ही चलता है। आधुनिक सभ्यता, जो शहरियत की द्योतक है, सर्वसाधारण की दुर्दशा की पूरी ज़िम्मेदार है।
देश-देशान्तर का व्यक्ति मानसिक रूप से किसी हिंसक पशु से कम नहीं लगता। मौका मिलने पर, और अवसर प्राप्त होने पर कौन क्या कुछ कर गुज़रेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लायन्स क्लब का मेम्बर होने न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। हां, ये क्लबें उसे प्रोत्साहन ही नहीं देतीं, उसे अवसर भी प्रदान करती हैं कि वो खुल खेले।
“महाबली, हमारे प्रदेश में एक नरभक्षी सिंह ने आतंक मचा रखा है, और प्रजा आपसे सुरक्षा की अपेक्षा रखती है।”
“क्यों नहीं! यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी प्रजा के सुख-दुख का ध्यान रखें। महामंत्री, तुरन्त प्रबन्ध किया जाये कि उस नरभक्षी को और आतंक मचाने का मौका न मिले। यह हमारा आदेश है।”
तब आज जैसे बड़े-बड़े शहर नहीं होते थे। ज़्यादातर गांव और जंगल होते थे, तथा असभ्य मानी जाने वाली जातियाँ, मुनियों और आश्रमों के पास तक नहीं फटकती थीं। यहां तक कि हिंसक पशु भी उनको तंग नहीं किया करते थे। फिर भी समय के राजा और शासक जंगलों में हिंसक पशुओं का आखेट किया करते थे ।
परन्तु आज तो सभ्य सरकारें इन हिंसक पशुतुल्य व्यक्तियों को – जिनकी समाज में ख़ूब मान-मर्यादा है – पूरा आश्रय देती हैं। परन्तु किया क्या जाये! व्यवस्था ही बदल गई है। बड़े-छोटे, अनेकों शहर बस गये हैं, और नरभक्षक, जो केवल मनुष्यों का ही ख़ून पीते हैं, खुले आम घूम रहे हैं।
मानव अपने आचार-विचार से ही पहचाना जाता है। आत्म-संतोष के स्थान पर शारीरिक तथा मानसिक प्यास और सत्ता की लौलुपता बुझाने की सुविधा आज उभर कर सामने आ रही है – जिससे उन्हें आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक लाभ उठाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। आज एक सभ्य मनुष्य तन-मन से काम करे भी तो क्यों, जब कुछ करे-धरे बग़ैर ही बृजेश्वर दयाल जैसे व्यक्ति दोनों हाथों से इतना धन बटोर सकते हैं कि सरकारी ख़र्च निकालकर सात पुश्तों के लिये भी पर्याप्त हो!
क्षमा करना, मैं आक्रोश में कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया था, और मूल कहानी से थोड़ा हट गया हूं। परन्तु अब कहने लायक विशेष कुछ है भी तो नहीं !
बी. डी. गुप्त से मुझे अब और भी दुर्गन्ध आने लगी है। प्लेट को एक कोने में सरकाकर, मैं दुखी मन से होटल के बाहर निकल आया। मौसम में हल्की ठंडक थी और मस्तिष्क में गर्मी। संतुलन बनाने के लिये बाहर लॉन में घूमने लगा कि इतने में झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आई। – दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे, और मेरी तरह अन्दर घुटन महसूस करते हुए मेरे पीछे-पीछे बाहर निकल आये थे।
“चोर है साला” एक ने शराब की झोंक में कहा,”सारे शेयरों पर कब्ज़ा जमाकर बैठा है।”
दूसरे व्यक्ति ने झट जवाब दिया,”अरे यार, यह तो धन्धा है। चोरी काहे की! माल हो तो तुम भी शेयर ख़रीद सकते हो।”
अब मेरे कान खड़े हो गये। लगा कि वे गुप्ता के बारे में ही बात कर रहे हैं । न चाहते हुए भी मैं अपने को उनकी बातचीत सुनने से रोक नहीं सका ।
“धन्धा काहे का!” पहला व्यक्ति उबल सा पड़ा,”सरासर धोखेबाज़ी है। पता नहीं क्यों बोर्ड के लोग इसको बर्दाश्त किये हुए हैं। मेरा बस चले तो नंगा कर दूं साले को।”
“मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा कि तू क्यों उस से इतना नाराज़ है! तेरा तो लंगोटिया है वो! ज़रा मंदी आई तो रोने लगा?”
“रोना तो यार तकदीर का है। इन्हीं दिनों तीस लाख डुबो चुका हूं। मुसीबत तो यह है कि जब कभी चार पैसे कमाने का मौका आता है, यह साला टपक कर टांग खींच लेता है। जाने कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा!”
दूसरे ने कहा, “तकदीर तो अपनी भी ख़राब ही है। दो दिनों में बीस टके का माल दस टके में कोई नहीं पूछता। शुकर है, हाथ में माल कम है। मैंने भी सोच लिया है कि चाहे सारा लुट जाऊं, इतने मंदे में तो हाथ नहीं खीचूंगा।”
“तुम्हारे पास तो बहुत शेयर थे! कब निकाले?”
“मैने तो ऐक्सचेंज में कह रखा था, गुप्ता बेचे तो बेच, और ख़रीदे तो ख़रीद। इसलिये समय रहते ही निपट लिया। चार दिन रुक जाता तो मैं भी गया था।”
“गुप्ता के पास तो अब भी काफ़ी माल है। वो भी तो भुगत रहा है।”
“ख़ाक भुगत रहा है! यह सब पैंतरेबाज़ी है। जानबूझकर कम्पनी डुबोता है और भाव गिरते ही दोनों हाथों से समेट लेता है। माल तो आसामियों का है। इसका क्या जाता है! कम्पनी पर अपनी पकड़ मज़बूत किये जा रहा है।”
मैं स्तब्ध रह गया कि क्या ऐसा भी होता है! या हो सकता है! मेरी विचारधारा अब गुप्ता से हटकर देश की अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ गई। सोचने लगा, इस देश को स्वतंत्र हुए पचास साल होने को आये परन्तु ग़रीब और ग़रीब तथा अमीर, और अमीर क्यों होता जा रहा है? देश मंहगाई से दबा जा रहा है तो इसका उत्तरदायी कौन है? – यह तब की बात थी जब मुझे अशोका में डिनर का निमंत्रणपत्र प्राप्त हुआ था।
आज दूरदर्शन पर पुरस्कार वितरण का समारोह है। देश के माने हुए उद्योगपतियों को सम्मानित किया जा रहा है। और हरियाणा बेस मैटल्स् तथा मिनरल्स् लिमिटिड के चेयरमैन श्री बी. डी. गुप्त को एक बड़ा सा प्रमाणपत्र और राशि पूज्य राष्ट्रपति के द्वारा दी जा रही है। कोई वजह नज़र नहीं आ रही, परन्तु मुझे सामने मेज़ पर पड़े टेलिविज़न से ही दुर्गन्ध आने लगी है। लेकिन टेलिविज़न तो मेरा अपना है! धीरे-धीरे, किसी न किसी दिन, यह गन्ध समाप्त हो ही जायेगी। ऐसी मेरी आशा है।
समाप्त
लेखक :- जगदीश लूथरा ‘नक्काद’