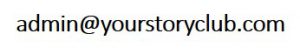परिचय – Introduction : (In this Hindi article, writer is searching for his identity and introduction as he is not finding himself suitable for different criteria of society.)

Hindi Article – Introduction
Photo credit: alive from morguefile.com
‘गधा – पाजी – नामाकूल’ ये शब्द हैं, स्वर्गीय पिताजी के जिनका प्रयोग वे प्राय: हर रोज़ मुझे डांटते फटकारते समय किया करते थे । और मैं इन शब्दों को सुनने का अभ्यस्त सा हो गया था ।
आज जब कि मैं लेखन जगत में परिचय हेतु जीवन में पहली बार लेखिनी उठा रहा हूं तो अपना कर्तव्य समझता हूं कि निसंकोच पूज्य पिताजी के विचार, जो उनके मेरे प्रति थे, उन्हीं के शब्दों में पाठकों के समक्ष ज्यों के त्यों रख दूं, ताकि मुझे समझने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।
कहते हैं कि ‘होनहार बिरवान के होत चीकने पात’, अर्थात व्यक्ति अपने जीवन में क्या कुछ कर गुज़रेगा, उसकी झलक उसके बाल्यकाल में ही मिल जाती है । माता-पिता चूंकि व्यक्ति के बाल्यावस्था तथा लड़कपन तक विशेष रूप से संरक्षक होते हैं और अपनी संतान को दूसरों की अपेक्षा भली भांति जानते हैं, इस कारण उनकी राय सत्य और मान्य होनी चाहिये । माता तो हो सकता है, मोहवश संतान को आंकने में कहीं चूक कर भी जाये, परन्तु पिता, जिसकी सभी आकांक्षायें हाड-मांस के उस पुतले के साथ सदैव जुड़ी रहती हैं, अपनी सूझ-बूझ के अनुसार उसके आंकने में कदाचित भूल नहीं कर सकता । विपरीत इसके उसकी विशेषताओं को बढ़ा-चढ़ा कर बखान करने में गर्व का अनुभव करेगा – यदि ऐसा कुछ बखान करने योग्य हो तो । संभवत: मेरे पिताजी भी मुझसे बहुत कुछ आशायें रखते होंगे, जिनको दुर्भाग्यवश मैं पूरा नहीं कर पाया । मुझे यह कहने में थोड़ा संकोच अवश्य हो रहा है किन्तु सत्य यही है कि वे मुझसे सर्वथा असंतुष्ट ही रहे ।
आप सोचते होंगे कि मैंने परिचय का यह अनोखा ढंग क्यों अपनाया है ! मुझे जो कुछ कहना है, सीधे सादे शब्दों में क्यों नहीं कहता । मैं मानता हूं कि एक कहानीकार के नाते इस तरह अपने पात्रों के मुख से सब कुछ उगलवाना काफ़ी सरल होगा और अपनी लघु-कथाओं में अपने विचारों को मैं भी उन्हीं के द्वारा कहूंगा । परन्तु यह मेरा वास्तविक परिचय तो न हुआ ! पात्र सत्य नहीं होते । और आवश्यकतानुसार लेखक की इच्छा से ही जीते या मरते हैं । वे सत्य भी कह सकते हैं और असत्य भी । वे तो वही कुछ कहते हैं जो लेखक उनसे कहलवाना चाहता है । परन्तु वो सब कुछ जो वास्तविक है, और लेखक के अन्त:करण में निहित है, उसे कौन कहेगा ! वे सब सत्य जो किन्हीं दुर्लभ क्षणों में एक झरने के समान फूट पड़ता है – केवल अन्त:करण की आवाज़ जिसे शब्दों में लाना कठिन होता है । जैसे :-
‘नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश सकल सुर त्रासा ।
सहज भाव प्रिय तामस देहा, जैसे उलूक हीं तम पर नेहा ।।’
रामायण का यह दोहा मुझे बहुत प्रिय है । जैसे आत्मा की गहराईयों से कुछ फूट निकला हो।
मेरे मन में एक मौलिक प्रश्न उठता है कि आख़िर एक लेखक लिखता है तो क्यों लिखता है! सफल लेखकगण मेरी धृष्टता क्षमा करें, मेरा विचार है कि सफलता अथवा असफलता तो बाद की बात है, जिसका मूल्यांकन समय, तथ्यों अथवा मानस की रुचि के अनुसार होता है । मूल रूप से तो लेखक एक हारा हुआ असहाय व्यक्ति होता है जो कुछ विशेष और इच्छा के अनुसार न कर पाने की अवस्था में अपना रोष लेखन द्वारा प्रकट करता है । यदि उसमें ग्रह-स्थिति के विपरीत संवेदन शक्ति और बुद्धि के साथ साथ थोड़ा मानसिक बल और संकल्प की दृढ़ता भी होती तो वो एक लेखक, एक कवि अथवा चित्रकार न होकर एक प्रखर नेता और विपरीत परिस्थितियों में एक विघटन-कारी व्यक्ति होता, जो समस्त समाज के लिये चुनौती सिद्ध होता ।
प्रकृति का नियम है कि जिस प्रकार हिंसक जीव आक्रमण करते हैं, सांप फुंकारते हैं, सींगधारी सामने से प्रहार करते हैं और गधा पीछे से दुलत्ती झाड़ता है, इसी प्रकार अपने चरित्र तथा संस्कारों के अनुरूप लेखक अच्छे अथवा बुरे लेख लिखते हैं, जिनकी ख्याति समय, समाज तथा प्रचलित विचारधारा के अनुसार होती है । और कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि लेखक का अपना चरित्र उसके लेखन में उभर कर सामने आ जाता है और जनता से कई बार काफ़ी प्रशंसा बटोर लेता है ।
बहुत समय से परिचय के लिये दो पद्यतियों का प्रयोग किया जाता रहा है । एक तो यह कि कोई व्यक्ति विशेष जिसको समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो, अथवा राजनेता हो, अपनी जानकारी के अनुसार जो आम तौर पर बहुत कम अथवा न के बराबर होती है, किसी लेखक के लिये कुछेक निजी कारणों से अथवा सेवाओं के बदले झूठमूठ प्रशंसा के चार शब्द कह दे कि अमुक व्यक्ति ने अथवा उसके विचारों ने उसे इतना प्रभावित किया है कि वो उसकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता, और चाहता है कि जनसाधारण भी लेखक के विचारों से लाभ प्राप्त करें । और ऐसे ही कुछ और शब्दों के साथ शुभकामनाओं सहित अपने पद तथा कार्यालय की छाप लगा देता है । इससे लेखक को लेखन बेचने में अथवा रॉयल्टी प्राप्त करने में सुविधा होती है । ये तो रहे मान्यताप्राप्त लेखक । दूसरी श्रेणी में वे लेखक आते हैं जो अपने विचारों को किसी जानी पहचानी अनुभूति के सर मढ़ कर बड़े नम्र भाव से और विशेष भावुक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने लेखन में प्रस्तुत करते हैं कि चाहे साधारणत: जनता उनको कदाचित स्वीकार न करती परन्तु अज्ञानता और अन्धविश्वासों के कारण मान लेती है कि सम्भवत: वह विषय उनकी बुद्धि से ऊपर की चीज़ है । हमारे धर्माचार्य, साधु, सन्यासी, पंडित, पादरी, मियां मौलाने इस पद्यति द्वारा ख्याति प्राप्त कर लेते हैं।
अपने बारे में ‘हम’ यह सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि हमारे लिये ये दोनों पद्यतियाँ उपयुक्त नहीं हैं । क्योंकि ‘हम’ अपने विचारों में अलौकिक तथा सबसे पृथक दृष्टिकोण रखते हैं । ‘हमारी’ धारणा है कि अभी तक समाजशास्त्रियों ने, अथवा विचारकों ने – जितनी जानकारी ‘हमें’ प्राप्त है – ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसका आज तक अनुसरण न होता आया हो । मगर समाज की दशा दिन-प्रतिदिन गिरती ही जा रही है । ‘हमारा’ विचार है कि इसमें मूल रूप से परिवर्तन की आवश्यकता है। हां, परिचय की पहली पद्यति ‘हमारे’ कुछ काम आ सकती है, परन्तु ‘हम’ तो ख़ुद ही स्वीकार कर चुके हैं कि लेखन जगत में यह ‘हमारा’ प्रथम प्रयास है । इसलिये जनसाधारण को तो ‘हमारे’ विचार जानने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ । हां, कुछ लोग ‘हमारे’ विचारों से भली भांति परिचित हैं और समाज में ऐसी स्थिति में हैं कि ‘हमारे’ विषय में बहुत कुछ कह सकते हैं । परन्तु ‘हमें’ नहीं लगता कि वे ऐसा कुछ करेंगे । क्योंकि :
‘हरचन्द कि आईना हूं पर इतना हूं नाकबूल ।
मुंह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करें ।।’
‘हम’ जन्म से राजपूत होते हैं । और वे विशेषतायें, गुण, अवगुण, जो किसी जाति से सम्बन्धित माने जाते हैं, ‘हम’ में उत्तम स्तर पर विद्यमान हैं । जैसे प्राप्त सुविधाओं और अधिकारों से सर्वदा असंतुष्ट रहना, न ख़ुद चैन से बैठना, न किसी को बैठने देना इत्यादि । वैसे पिछली कई पीढ़ियों से मेरा राजपूताना से नाता नहीं रहा, और न ही मेरे बाप-दादा ने विशेष रूप से मुझे बताया ही है कि ‘हम’ जाति से राजपूत हैं, परन्तु मैंने अपने तौर पर खोजबीन करके यह जान लिया, अथवा मान लिया है कि ‘हम’ राजपूत ही हैं । और हमारे पूर्वज किन्हीं विशेष कारणों से अपने मूल स्थान से पलायन करके पंजाब के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में आ बसे थे । उन्होंने राजपूत कहलाना क्यों पसन्द नहीं किया, यह मैं नहीं जानता । परन्तु मेरी बात का खंडन भी हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया । उर्दू में कहावत है ‘तुख़म-ए-तासीर, सोहबत-ए-असर’ । ‘हमने’ अपने तथा सगे सम्बन्धियों के स्वभाव, पहरावे तथा खान-पान से जान लिया है कि हम राजपूत ही हैं । वैसे मैं जात पात में विश्वास नहीं करता परन्तु अपनी जात-बिरादरी में मैंने यह जाना है कि क्रोधान्ध तथा सर्वदा बिखराव की स्थिति में रहना और नितान्त संघर्ष करते रहना हमारे सामाजिक जीवन का एक अंग रहा है । स्वभाव से पूज्य पिताजी भी गुस्सैल और प्राय: व्यग्र प्रकृति के व्यक्ति थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाना और बच्चों के व्यवहार से कभी संतुष्ट न होना उनका स्वभाव ही था । इस कारण वे मुझे अक्सर डांटते फटकारते रहते थे ।
बड़े बूढ़े यदि अपने मन्द-बुद्धि बच्चों के लिये उल्लू, गधा, पाजी जैसे शब्दों का प्रयोग करें तो इसमें बताने लायक तो कुछ नहीं है, और पिताजी ने भी मुझे ऐसा कुछ कह दिया हो तो कुछ आश्चर्यजनक नहीं । परन्तु उक्त शब्दों के साथ नामाकूल शब्द का प्रयोग करना, जिसका मैं बहुत समय तक अर्थ भी न जान पाया, न जाने क्यों मेरे मन-मस्तिष्क के किसी कोने में ऐसा अटक गया कि मेरे जीवन का अंग ही नहीं, सम्पूर्ण जीवन ही बन कर रह गया है ।
स्पष्ट है कि यह शब्द मातृभाषा का तो नहीं । और न ही हमारे प्रदेश में बोली जाने वाली पंजाबी का है । परन्तु जिस प्रकार आजकल के पढ़े लिखे व्यक्ति क्रोधावस्था में अंग्रेज़ी का कुछ अधिक ही प्रयोग करते हैं, पूज्य पिताजी – जो अपने समय में प्रचलित उर्दू-फ़ारसी के अच्छे विद्वान थे – स्वाभाविक रूप से इस शब्द का प्रयोग करते होंगे । परन्तु प्रश्न भाषा का नहीं, अपितु धारणा का है, जो उनकी मेरे प्रति थी । नक्कादुल-लुग़ात के अनुसार नामाकूल का अर्थ है – नावाजिब या नामुनासिब । और सरल हिन्दी में – जो उपयुक्त न हो अथवा सर्वमान्य परम्पराओं तथा धारणाओं के विपरीत हो और अनुकूल न हो, उसे नामाकूल कहते हैं । जिसको अंग्रेज़ी भाषा में Misfit कहा जाता है, और दुर्भाग्यवश ‘हम’ समूचे जीवन के किसी काल में कहीं फ़िट नहीं बैठे । ऐसा नहीं कि ‘हम’ समय और समाज की विचारधारा को समझने की योग्यता नहीं रखते, परन्तु जैसा मैंने पूर्व कहा है कि ‘हम राजपूत होते हैं’ और आस्तित्व की अपेक्षा ‘हमें’ मूंछों का अधिक ध्यान रहता है । इस कारण ‘हम’ सदा असफल रहे । और इसी मूल कारण से ‘हम’ आज लेखन जगत में प्रवेश करने जा रहे हैं । अपने विचारानुसार अपनी बात को खुले आम कहने का साहस भी है और विपरीत परिस्थितियों में रहने की आदत भी है । परन्तु –
‘क्या बतायें उम्र भर की काविशों के बावजूद ।
दौर-ए-नाहंजार के हमसे न पेच-औ-ख़म गये ।।’
हम जिस वातावरण में सांस लेते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिये – जो दम घुटने से पहले चिल्लाने की क्षमता रखता हो, और मुंह में ज़ुबान भी रखता हो – नेतागिरी के कीटणुओं से प्रभावित अथवा ग्रस्त हो जाना संभव है । ‘हम’ भी इस बीमारी से न बच पायें तो कुछ आश्चर्यजनक नहीं है ।
लड़कपन में तो कुछ उल्लेखनीय नहीं था । शिक्षापूर्ति के बाद ‘हमारी’ पहली नियुक्ति एक मिलिट्री वर्कशॉप में हुई । और बहुत जल्द अपने अड़ियल रवैये के कारण प्रशासन की नज़र में खटकने लगे । परन्तु श्रमिक वर्ग में पहचाने जाने लगे । एक श्रमिक संगठन संवैधानिक औपचारिकतावश चल रहा था । ‘हमें’ नेता बनने में विशेष कठिनाई नहीं हुई । परन्तु – पिताजी के कथनानुसार – ‘हमारी नामाकूलियत’ आड़े आई और जहां ‘हम’ से पूर्व संगठन के नेता तालमेल बिठाकर पदोन्नत्ति प्राप्त करते थे, ‘हमें’ सबसे नीचे के स्तर से उठने नहीं दिया गया । श्रमिकों के लिये तो ‘हम’ कुछ विशेष सुविधायें न जुटा पाये, प्रशासन से बैर मोल ले बैठे । बात इतनी सी थी कि मैं संवैधानिक धाराओं के अनुसार संगठन को राष्ट्रीय स्तर के संगठनों से जोड़ना चाहता था, जो प्रशासन के हित में नहीं था । इससे आगे चलकर उसके लिये कई एक कठिनाईयां उत्पन्न होने की आशंका थी । अलबत्ता श्रमिकों को अवश्य बल मिलता । एक सोची समझी चाल के अन्तर्गत मार-पीट के आरोप में ‘हम’ नौकरी से निकाल दिये गये ।
आप यह न सोच लेना कि जीवन की इस पहली असफलता के पश्चात् ‘हमने’ नेतागिरी से तौबा कर ली ! ‘हमारी’ दूसरी और अन्तिम नियुक्ति रेलवे में थी जहां ‘हमारे’ खुल-खेलने के लिये सुव्यवस्थित श्रमिक संगठन तथा अनुकूल वातावरण था । मान्यताप्राप्त संगठनों के अतिरिक्त कई- एक और भी संगठन मौजूद थे । परन्तु उनमें प्राय: सभी किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए ही नहीं थे बल्कि उन्हीं से संचालित थे । अब ‘हमारी’ समझ में आया कि प्रशासन से टक्कर लेने के लिये राजनीतिक संरक्षण लेना ही पड़ता है । मगर व्यक्तिगत अनुभव से ‘हमने’ जान लिया था कि श्रमिकों की मांगों की आड़ में राजनीतिक खेल खेलने के लिये श्रमिकवर्ग का तो केवल दुरुपयोग ही होता है । श्रमिक कुछ पाने की लालसा में संघर्षशील होते हैं और विघटनकारियों के हाथों में खेलने लगते हैं । आज तक प्रशासन द्वारा श्रमिकों का जितना भी उत्पीड़न हुआ है, उससे आधे का लाभ भी ये संगठन नहीं दिलवा पाये । देश के साधनों का नुकसान तो होता ही है, श्रमिकों का कुछ भला भी नहीं होता ।
कोई पूछे कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है ! ‘हम’ अपने ही संगठन के प्रधान के समक्ष खड़े हो गये और एक मीटिंग में अध्यक्ष महोदय से मांग कर बैठे कि प्रशासन से लड़ाई मोल लेने से पूर्व श्रमिक संगठनों का एकीकरण किया जाये ताकि प्रशासन श्रमिकों को उत्पीड़ित न कर सके । इसके लिये कोई सूत्र ऐसा भी हो जिससे आन्दोलन राजनीतिज्ञों की अपेक्षा संगठनों की निर्वाचित समिति के हाथ में रहे । ऐसी व्यवस्था तो की गई, लेकिन दिखावेमात्र के लिये ही । सत्ताधारी पक्ष से जुड़े श्रमिक संगठन ने आम हड़ताल का डटकर विरोध किया । इस समस्या को सुलझाने के लिये ‘हम’ कई-एक साथियों को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, चाणक्यपुरी जा पहुंचे कि बीच-बचाव करके उत्तर रेलवे मज़दूर संघ के साथ श्रमिक हित में समझौता हो सके, जो राजनीतिक दृष्टि से बचकाना हरकत थी क्योंकि हड़ताल श्रमिकों की मांगों को लेकर नहीं थी, बल्कि इंदिरा जी को सत्ता से हटाने के लिये की जा रही थी जिसमें राष्ट्रबन्धु श्री जयप्रकाश जी की मरज़ी भी शामिल थी । इसलिये ‘हमें’ दो-एक बार मज़ाक का निशाना भी बनना पड़ा । यह ‘हमारी’ श्रमिक कल्याण के हित में किये गये संघर्ष की अन्तिम पराजय थी । अब तो आप जान ही गये होंगे कि परिचय की पहली पद्यति ‘हमारे’ लिये उपयुक्त क्यों नहीं है !
‘ता उम्र काविशों का महासल यह बेकसी ।
ए काश जान पाते यह सब इब्तदा से हम ।।’
मेरे विचार प्रचलित पद्यति तथा निर्धारित सामाजिक रूपरेखाओं के विरुद्ध क्यों रहे हैं, चलते चलते अपने जीवन के बाल्यकाल की एक घटना से आरम्भ करता हूं – यदि आप बोर न हो गए हों तो ।
एक दिन भारी भरकम बस्ता पीठ पर लादे, कड़कती दोपहर में – स्कूल से छुट्टी के बाद – मैं घर जा रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मुझे उछाल दिया और मैं मुंह के बल पृथ्वी पर धूल चाटने लगा । किसी साईकिल सवार ने मुझे पीछे से टक्कर मार दी थी । इस से पूर्व कि मैं सम्हल पाता, वो अपनी साईकिल तेज़ी से चलाता हुआ दूर मोड़ पर मेरी आँखों से ओझल हो गया । मेरे दिल में कसक रह गई कि काश! वो भी गिर जाता तो कम से कम मैं उसको देख तो लेता ! गुस्सा तो मुझे बहुत आया परन्तु ऐसी दयनीय स्थिति में मैं कर भी क्या सकता था ! इस घटना की छाप मेरे मस्तिष्क पर ऐसी पड़ी कि मैंने सीधे रास्ते चलना ही छोड़ दिया । उम्र के साथ-साथ इस घटना के विषय में मैंने कई पहलुओं पर विचार किया है। कई वर्ष बाद जो विचार मेरे मस्तिष्क में उभर कर आया है कि प्रगति का यह अर्थ कदाचित नहीं कि दूसरों को गिराकर धूल चाटने के लिये पीछे छोड़ दिया जाये जिससे कि जन-साधारण आप तक पहुंचने में हांफने लगे । यही मूल कारण है समाज में उभरती हुई विषमताओं का । इसी से वर्ग-संघर्ष बढ़ता है और शान्ति भंग होती है । मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे सरल विचार – सरल जीवन जीने के – मेरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के थे कि एक वर्गहीन समाज की रचना हेतु मशीनों का प्रयोग न किया जाये । इस देश का कल्याण मशीनों से नहीं, अपितु अधिक से अधिक श्रम-शक्ति के आधार पर – जनसाधारण के लिये उपयुक्त – उत्पादन से ही है ।
मैं उन दिनों सरगोधा शहर में कालेज में पढ़ता था । मुस्लिम लीग के अनुयायी मेरे कुछ सहपाठी कायदे-आज़म मुहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा को बढ़ा-चढ़ा कर बखान करते और गांधी बाबा की धोती का मज़ाक उड़ाया करते थे । मैं राजनीतिक समझबूझ तो कम रखता था मगर अक्सर उन से उलझ जाता कि जनसाधारण की वेशभूषा में रहने वाला संत व्यक्ति ही हमारा नेता हो सकता है, न कि पाश्वात्य शिक्षा तथा संस्कारों से ओत-प्रोत युवक जो धर्म के नाम पर देश का विभाजन चाहता हो । परन्तु मुझे क्या पता था कि केवल जिन्ना ही नहीं, गांधी जी के आसपास मंडराने वाले अधिकांश व्यक्ति बहुरूपिये हैं, जो सत्ता के लोभ में संगठन के साथ जुड़े हुए हैं । और यही हुआ भी । अधिकार प्राप्त होते ही गांधी जी के अमृत-तुल्य विचारों को ऐसे गंदे पात्र मिले जिसमें वो पवित्र विचारधारा विष के समान हो गई । नेता दोहरा जीवन जीने लगे । ‘त्यागी जी’ की धन-समृद्धि में बढ़ोतरी तथा ’ब्रह्मचारी जी’ की संतान में वृद्धि होने लगी । परन्तु ऐसा कुछ नया नहीं हुआ जो इतिहास में पहले न हुआ हो । हां, सदियों बाद मानव-कल्याण का सपना आँखों में समोये एक युगपुरुष का प्रयास फिर असफल हुआ था । तब से मैं जनकल्याण के किसी भी राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रयास को शंका की दृष्टि से देखने लगा हूं ।
एक सार्वजनिक स्थान पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था । उसपर एक मुर्गी का चित्र बना था जो ढेर सारे अण्डे दे रही थी । नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था ‘अधिक उत्पादन कीजिये’ पहले तो मुझे चित्रकार के दृष्टिकोण पर हैरानी हुई कि इतनी जनसंख्या के होते हुए भी वो उसे और क्यों बढ़ाना चाहता है ! फिर अपनी ही विचारधारा पर हंसी आ गई । मैं गम्भीरता से सोचने लगा कि इसमें मुर्गी का लाभ है या देश का ! क्योंकि मुर्गी जितने भी अण्डे दे, उसे तो कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं । वो जब तक उत्पादन करती रहेगी, दाना मिलता रहेगा । और फिर एक न एक दिन किसी डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा रही होगी । चूंकि मुर्गी और उसके अण्डे खाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है – आज़ादी मिलने के बाद से – इसलिये उत्पादन पर ज़ोर दिया जा रहा है और राजतंत्र भी इसे प्रोत्साहित कर रहा है । कल जब अण्डे अधिक, और खाने वाले कुछ कम होंगे तो अण्डों का भाव गिर जायेगा । और फिर उस समस्या को सुलझाने के लिये एक दूसरा बोर्ड लगा होगा जिसमें शायद लिखा हो ‘हम दो – हमारे दो’ । प्रश्न तो अब भी वही है । पर मुर्गी पर कौन सा संविधान लागू होता है ! यदि देश की समस्या है तो सुलझाने के लिये केवल दो तक परिवार सीमित रखने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि वे बच्चों के पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा का पूरा भार उठाने के लिये सरकार से पूरा आश्वासन प्राप्त करें । उद्योगपतियों के हित में तो यह है कि अण्डे अधिक हों ताकि वे स्वस्थ अण्डे कम दामों में पा सकें । बाकी अधिक उत्पादन की समस्या उनकी नहीं । और सरकार तो अपना ‘दायित्व निभाने के लिये’ बोर्ड लगवा ही देगी कि ‘कृपया उत्पादन कम कीजिये’ ।
आज अधिक उत्पादन से पाश्चात्य जगत बेहद दुखी है इसलिये वहां श्रम के समय में कटौती और मज़दूरी के साथ छुट्टियों की व्यवस्था भी की गई है। जैसे-जैसे कम्प्यूटर का प्रयोग बढ़ रहा है, श्रमिकों की आवश्यकता कम होती जा रही है । जल्द ही वो समय भी आयेगा जब यही लोग – जो आज अण्डे छांट कर लेते हैं – अण्डों को किसी भी भाव ख़रीदने को तैयार नहीं होंगे । यह होगी कम्प्यूटर युग की अन्तिम देन । विकसित देश अपने श्रमिक वर्ग को उचित मज़दूरी देकर औद्यौगिक स्पर्धा के इस युग में नहीं टिक सकते । इसी कारण पूर्वी देशों में सस्ती मज़दूरी का लाभ उठाकर हमारी ही औद्यौगिक प्रगति के आड़े आ रहे हैं । इसी सम्भावित स्थिति का अनुभव करते हुए गांधी जी ने स्वदेशी की दुहाई दी थी । हम ख़ुद अपने ही हाथों पिछले पैंसठ वर्षों के किये पर पानी क्यों फेर रहे हैं, मेरी समझ से तो बाहर है । विषय क्योंकि व्यापारिक तथा अर्थ से जुड़ा हुआ है, मैं ज़्यादा न कह कर विषय पर पुन: ध्यान देने का अनुरोध अवश्य करूंगा ।
अब बात चल ही निकली है तो यह भी चाहूंगा कि श्रमिक वर्ग – ख़ास तौर पर असंगठित वर्ग – के साथ भी न्याय होना चाहिये । उस की दशा भी दयनीय है । आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर काम पाने वाले व्यक्ति, जो सरकारी विभागों में ठेकेदारों के साथ – और एक बड़ा वर्ग राम भरोसे – हर रोज़ घूम फिर कर काम जुटाने का प्रयास करते हैं । उन के लिये – मिल जाये तो ईद, न मिले तो रोज़ा । उन्हें अधिकतर रोज़ा ही रखना पड़ता है क्योंकि बहुत से बहुत महीने भर में पन्द्रह-बीस दिन ही काम मिलता है । अपने देश के कर्णधारों के लिये यह लज्जा का विषय है कि वे स्वाधीनता के पैंसठ वर्ष बीत जाने पर भी उन के लिये इतना काम नहीं जुटा पाये कि जीवन की बाकी आवश्यकतायें पूरी करना तो एक तरफ़, वे अपना तथा अपने परिवार का पेट भर सकें ।
हम अपनी उपलब्धियों का बखान करते नहीं थकते । परन्तु यदि कुछ उपलब्धि है भी तो समाज के मध्यम तथा उच्च-मध्यम वर्ग के लिये – जिनका जीवन भी पहले की अपेक्षा अभावग्रस्त है । बाकी तो चारों तरफ़ समस्यायें ही समस्यायें हैं ।
‘आईने अहले सियासत को मुबारकबाद दें,
ज़िन्दगी में कुछ नहीं छोड़ा मसायल के सिवा ।
मुत्तफ़िक इस पर सभी हैं – क्या ख़ुदा क्या नाख़ुदा,
अब सफ़ीना और कहीं भी जाये साहिल के सिवा ।।’
आप अभी तक जनता जनार्दन के लिये – जिनके पूर्वजों के त्याग और बलिदान के फलस्वरूप आपको यह विशाल उपभोक्ता क्षेत्र प्रदान हुआ है और जिसका अभी तक आप सभी ने व्यक्तिगत लाभ उठाया है – पीने लायक पानी तक जुटा नहीं सके । क्योंकि दुर्भाग्यवश मैं यहां का नागरिक हूं, इसलिये यह कहने में थोड़ी झिझक हो रही है कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य दूसरे महायुद्ध से आर्थिक विवशता तथा इस देश का उपभोक्ता क्षेत्र पाने को लालायित दूसरे राष्ट्रों के हाथों विवश न होता तो यहां का उद्योगपति – जिसने अपने लिये यह लाभ उठाने के हेतु स्वाधीनता के आन्दोलन को आर्थिक सहायता दी थी – घुटनों पर सिर रखे बैठा होता । यह तो – संयोगवश – अवसर आपके हाथ लगा है । कोई भी बूढ़ा – जिसने वो राज भी देखा था – अपनी छाती पर हाथ रख कर कह देगा कि आज की अपेक्षा तब जनसाधारण अधिक सुरक्षित और सुखी था । अपनी भावुकता के कारण मैं अपने उद्गारों को व्यक्त किये बिना भी नहीं रह सकता ।
गत पैंसठ वर्ष के लम्बे अर्से में मैंने पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी तथा अवसरवादी, कई सरकारों को आते जाते देखा है जिन्होंने वायदों के नाम पर विवादों को जन्म दिया, अपनी स्वार्थ-पूर्ति की, परन्तु किसी ने भूले से भी उस निस्सहाय व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा जो आजतक आँखों में सुख से जीने के सपने लिये उनकी ओर देख रहा है । उन्होंने यह समझने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की कि उसकी भी कुछ आवश्यकतायें हैं ।
मैं नहीं कह सकता कि सरकार की क्या मजबूरियां रही होंगी । परन्तु यदि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारानुसार व्यक्ति को अपने श्रम का स्वामी बनने का अवसर दिया जाता और तीन-चार पंचवर्षीय योजनायें कृषि पर ही आधारित होतीं तो प्रति-व्यक्ति आय में संतोषजनक वृद्धि होती । परन्तु कर्णधारों को तो पहले उद्योगपतियों का आभार चुकाना था और उनको अपनी पूंजी को शीघ्रातिशीघ्र बटोरना भी तो था ! जनसाधारण को केवल एक अवसर पर्याप्त था । राष्ट्र, समाज, सम्प्रदाय, धर्म, सबका मूल आधार व्यक्ति है । किसी भी समाज तथा राष्ट्र की प्रगति का माप-दण्ड भी यही है कि वहां का साधारण व्यक्ति कितना सुखी और सुरक्षित है । यदि व्यक्ति को सद्भावना से कार्य में समान अधिकार देकर प्रगति में साझीदार बनाया होता तो जितना योगदान देने पर वो बाध्य है, स्वेच्छा से देश के लिये वो सब कर गुज़रता, जिसका आने वाली सन्तति आभारी रहती और देश वास्तविक रूप से सोने की चिड़िया होता ।
अब तो लगता है कि उद्योगपतियों तथा उनका समर्थन करने वाले प्रशासन ने सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी की ही हत्या कर दी है । वो अब मांस का एक टुकड़ा है जिसका उपभोग कोई कब तक करेगा !
नैतिक आधार पर सोचा जाये तो, क्या अधिकार है एक मानव का दूसरे मानव को अपनी निजी सेवाओं के लिये भोगने का ! मानवता तो पशुओं के साथ भी दुर्व्यवहार तथा अत्याचार के विरुद्ध है । इन प्राणियों का दोष केवल यही तो है कि उनका जन्म आपके घर न होकर किसी गरीब की झोंपड़ी में हुआ है । सारा जीवन तो वो आपकी सेवा करे, और वृद्धावस्था तथा असमर्थता के कारण सड़क पर गले सड़े मांस के लोथड़े की तरह फेंक दिया जाये !
आज की व्यवस्था में एक विशेष स्थान है धर्माचार्यों का, जो मानव को मानवता-संदेश देने के बजाय अतीत के राम-राज्य के किस्से सुना सुना कर उनके अहम् को और उभारते हैं । मंदिरों तथा मस्जिदों के कलश उठाने से किसी का कल्याण नहीं होने जा रहा । ज़्यादा से ज़्यादा इन धर्माचार्यों को हलवा-मांडा प्राप्त हो सकता है ।
मुझे ज्ञात है कि ये खरी-खोटी बातें आपको अखरेंगी अवश्य । मगर सत्य यही है कि मैं पिताजी के कहे अनुसार ‘नामाकूल’ हूं । समाज में फ़िट नहीं बैठ पाऊंगा ।
__END__
लेखक :- जगदीश लूथरा ‘नक्काद’